जीवन की उत्पत्ति जाति- विद्वेष: सभ्यताएं भाग -1
On

डॉ. चंद्र बहादुर थापा
वित्त एवं विधि सलाहकार- भारतीय शिक्षा बोर्ड एवं
विधि परामर्शदाता पतंजलि समूह
पृथ्वी भर में करोड़ों वर्षों से मानव, समूहों में, विभिन्न कारणों से, बसता-बिखरता रहा और अपने अपने समूहों के उत्थान-पतन के साथ साथ अनुवांशिक संततियों को पीढ़ी-दर-पीढ़ी विशिष्ट अथवा साधारण, शासक अथवा शासित, इत्यादि के रूप में जीवंत रखने की कोशिश में अपने अपने रहन-सहन, आचार-व्यवहार, आपसी सामाजिक अधिकार- कर्तव्य, अनुपालन और कोताही में पुरस्कार-दण्ड, के परिपाटियां चलाता रहा। भौगोलिक, राजनैतिक और प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न आपद-बिपद से उद्वेलित वातावरण को सहन कर जो भी समूह सफलतापूर्वक चला उसको आधुनिक शब्दों में उसके अच्छे दिनों को सभ्यता कहा जाता है और उसके लिखित-अलिखित प्रचलन को परम्परा। संसार के मानव सहित सभी जीवों के भलाई के लिए प्रयुक्त परम्परा को सनातन अथवा धर्म (विशेषकर प्राचीन भारतवर्ष, भारत खण्ड के समूहों में) और किसी विशेष समूह अथवा समूहों के संस्थापक के द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के आधार पर चलने वाले परंपरा को विशेषकर पश्चिमी समूहों में रिलिजन- Religion तथा अरब भाषी समूहों में ‘दीन- Deen, ग्रीक में प्रारम्भ में Ubesia और आधुनिक रिलिजन के अर्थ में Threskia,, इत्यादि से सम्बोधित किया जाता है।
वर्तमान काल में सनातन धर्म हिंदू का ही वैकल्पिक नाम है जिसका उपयोग संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं में भी किया जाता है। ‘सनातन’ का अर्थ है - शाश्वत या ‘सदा बना रहने वाला’, अर्थात् जिसका न आदि है न अन्त। वैदिक शास्त्रों में भारतीय उपमहाद्वीप के धर्म के लिए ‘सनातन धर्म’ नाम मिलता है। सनातन धर्म वास्तव में सामाजिक व्यवथा में ब्रह्माण्ड अवस्थित सभी अवयव, निर्जीव-जीवित पदार्थ सहित प्राणियों के उत्कृष्ट स्वरूप मनुष्य सहित उनके पूर्वजों के उत्थान कैसे हो सम्बन्धी अनुभव के भावी संततियों के लिए छोड़े गए व्यव्हार सूत्रों और दिशानिर्देशों के संकलन है जो प्रारंभ में अपने-अपने समूहों में वातावरण सहित भौगोलिक परिस्थिति अनुरूप जलवायु अनुकूलन अनुसार रहन-सहन और आत्म सुरक्षा के साथ आत्म उत्कर्ष के लिए अपनाये जाने हेतु पृथ्वी के कोने-कोने में फैलते हुए पहले श्रुति-स्मृति और बाद में पत्थर, धातु-पत्रों, फिर भोजपत्रों और धीरे-धीरे कागज में हस्तलिखित, फिर टंकण और वर्तमान में संचार-साधनों के विभिन्न माध्यम से डिजिटल स्वरूप में संजोया और संरक्षित किया जा रहा है, और प्रलयकाल तक क्या रूप होगा नहीं मालूम। क्योंकि ये सामग्री संस्कृत, पाली, तमिल, तेलगु, सहित वृहद भारत के प्राचीन भाषा में हैं, इसीलिए इसे भारतीय बोला गया है। पृथ्वी के जिस भौगोलिक क्षेत्र में जो मानव समूह अपने आचार-व्यव्हार के लिए जो भाषा प्रयोग करता है उसी भाषा में अपने सामाजिक ताने-बाने सहित सामाजिक नियम के लिए सूत्रों और दिशानिर्देश बनाता है और मूलरूप से वहां के लिए वही सनातन धर्म बनता है क्योंकि वह वहां के लिए है, और उसी क्षेत्र का कहा जाता है। अत: सनातन, ईसाई और इस्लाम से पूर्व के सामाजिक व्यवस्था सम्बन्धी सूत्रों और दिशानिर्देशों के मानव समूहों के अलग-अलग प्रचलन के सामूहिक संकलन है चाहे जिस भाषा और चाहे पृथ्वी के जिस कोने में प्रचलन में हो और लिखा गया हो, चाहे आज के परिवेश में अच्छा लगे अथवा बुरा लगे।
वर्तमान में मुख्यरूप से संसार में चार प्रमुख समूह हैं जो सभ्यताओं के ही ध्वजवाहक हैं : (1) सनातन जिसमें - अखण्ड भारत में प्रतिपादित हिन्दू, जैन, बौद्ध, सिख के शाखा-प्रशाखा से विश्व में फैले और विश्व के कोने-कोने में अपने-अपने परंपरा मानने वाले मानव समूह आते हैं, (2) ईसाई - जिसकी प्रारम्भ की 2024वां वर्ष चल रहा है, इजराइल के वेतहेलम में जन्में इसा मसीह (जीसस क्राइस्ट) के सुसमाचार जो परमपिता परमेश्वर ने उनके पुत्र ईसा मसीह (यीशु मसीह) को दिये गये निर्देशों पर आधारित सुसमाचार फैलाने के लिए चयनित पवित्र आत्माओं के द्वारा चर्च के माध्यम से विश्व में ईश्वर के राज्य स्थापित करने के मिशन में लगे हुए ईसाई, वर्तमान में कैथोलिक, मैथोडिस्ट, प्रोटोस्टेंट मूल से विखंडित 43,000 से अधिक छोटे बड़े ईसाई समूह जाति-प्रजाति, (3) इस्लाम - जिसकी प्रारंभ की 355/356 दिन के वर्ष आधारित हिजरी 1445वां वर्ष चल रहा है, मक्का में कुरैश जनजाति की एक शाखा अदनानी बानू हाशिम कबीले के व्यापारी और मिट्टी के कारीगर पिता अब्दुल्लह इब्न अब्दुल मुत्तलिब और माता आमिना बिन्त वहब से 570 ईस्वी में जन्मे मुह़म्मद इब्न अ़ब्दुल्लाह अल हाशिम (हज़रत मोहम्मद) द्वारा प्रतिपादित कुरआन आधारित 72 फिरके से निकली 73वें फिरके के 533 से अधिक छोटे-बड़े समूहों वाला शिया, सुन्नी और सूफी वर्गों में विभाजित मुसलमान समूह, (4) कम्युनिज़्म के सिद्धान्त के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ने तैयार किया और 21 फऱवरी सन् 1848 को पहली बार जर्मन भाषा में प्रकाशित साम्यवादी घोषणापत्र से प्रतिपादित कम्युनिस्ट समूह जो मार्कि्सस्ट, लेनिनिस्ट, माओवादी मूल से देश और नेता के नाम से सैकड़ों उप-समूह में विभाजित नास्तिक समूह। और माने अथवा ना माने, ये ही सबसे बड़े आज के विश्व के मुख्य जातियाँ हैं, न कि तथाकथित हिन्दुओं के प्राचीन कार्य कौशल आधारित वैज्ञानिक वर्ग विभाजन को, अंग्रेजी शिक्षा नीति के पोषक आज के तथाकथित आधुनिक बुद्धिजीवियों के झुण्ड ने स्वार्थ आधारित उद्देश्य से दिया गया भारत के हिन्दुओं के ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य, शूद्र जातियां।
ईसाई से पहले के परंपरा (सभ्यता) पद्धतियां : सुमेर से सिंधु घाटी (1-8) की सभ्यता तक
वर्तमान युग में, आज से करीब पांच हजार वर्ष पूर्व विश्व के कई भागों में कई सभ्यताएं फल-फूल चुकी थीं। ये सभी सभ्याताएं सामान्यतया नदियों के किनारे विकसित हुईं। प्राच्य और पश्चिमी बुद्धिजीवियों द्वारा सन्दर्भित सभ्यताएँ जो भू-मध्यसागर के चारों ओर, सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों के तलहटियों के मैदान और मूल से आगे के रास्तों के घाटियों, उत्तर-अफ्रीका के अरब क्षेत्र, अफ्रीकी नील नदी के तलहटियों के मैदान, इत्यादि के आधुनिक युग के प्राचीनतम सभ्यताएँ मुख्यत: निम्न हैं -
(1) सुमेर सभ्यता - दक्षिणी मेसोपोटामिया का क्षेत्र, जो लगभग 5000/4500-1750 ईसा पूर्व में आधुनिक इराक और कुवैत के अनुरूप था। इस भूमि पर 4500 ईसा पूर्व से पहले अज्ञात मूल के लोग रहते थे जिन्हें पुरातत्वविदों ने उबैद लोग (अल-उबैद के स्थान के नाम पर जहां खुदाई में पहली बार उनके अस्तित्व का पता चला) नाम दिया है। लैंगडन के अनुसार मोहन जोदड़ो की लिपि और मुहरें, सुमेरी लिपि और मुहरों से मिलती हैं। सुमेर के प्राचीन शहर ऊर में भारत में चूने-मिट्टी के बने बर्तन पाए गए हैं। मोहन जोदड़ो की सांड की मूर्ति सुमेर के पवित्र वृषभ से मिलती है और हड़प्पा में मिले सिंगारदान की बनावट ऊर में मिले सिंगारदान जैसी है। इन सबके आधार पर कहा जा सकता है कि सुमेर और भारत में बड़े पुराने सम्बन्ध थे। सुमेर शब्द भी हमें पौराणिक पर्वत सुमेरु की याद दिलाती है। संसार की सबसे पुरानी लिपि का जन्म सुमेर में ही हुआ। गीली मिट्टी की पटिया पर कील जैसे औज़ार से गोद कर लिखी जाने वाली इस लिपि को कीलाक्षर लिपि कहते हैं। जिसे सबसे पहले हेनरी राँलनस ने पढा था। इस लिपि में संसार के सबसे पुराने व्यापारिक खाते बनाए गए और खातों में दुहरी प्रविष्टि या डबल एंट्री व्यवस्था का प्रयोग हुआ, जो आज तक प्रचलित है। इसी लिपि में प्राचीन कैलेंडर का भी निर्माण हुआ। बैंकिंग प्रणाली का जन्म मेसोपोटामिया में ही हुआ था। जिस स्थान पर ईसा से लगभग 37 वर्ष पहले मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किया था, वह यही था। जैसे हमारे पुराणों में जल-प्लावन की कथा आती है, जिसमें मनु बच गये थे, ऐसी कहानियाँ संसार के अन्य प्राचीन ग्रन्थों में भी मिलती हैं। मेसोपोटामिया में हज़ारों वर्ष पहले महाकाव्य रचने की प्रवृत्ति ने जन्म लिया था और यहीं गिलगमेश का महाकाव्य रचा गया था। राजा गिलगमेश के इस कीर्ति ग्रन्थ में इसी प्रकार के जल-प्लावन का भी उल्लेख है।
(2) मिनोआई सभ्यता - यह सभ्यता कांस्य युग में यूनान के दक्षिण में स्थित क्रीत के द्वीप पर उभरकर 27वीं सदी ईसापूर्व से 15वीं सदी ईसापूर्व तक फलने-फूलने वाली एक संस्कृति थी। यह यूरोप की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। इतिहासकारों को मिले साक्ष्यों से ज्ञात हुआ है कि मानव 1,28,000 ई.पू में ही आकर क्रीत पर बस चुके थे लेकिन यहाँ कृषि लगभग 5000 ई.पू में ही जाकर विकसित स्तर पर पहुँची। क्रीत के द्वीप पर बहुत से मिनोआई खंडर मिले हैं। यह महल, प्रशासनिक दफ़्तर, घर और दुकानों की श्रेणियों में देखें गए हैं। महलों में अक्सर दो या उस से भी अधिक मंजिलें मिली हैं। बड़े स्तम्भ, अन्दर और बाहर जीने (सीढिय़ाँ) और आँगन इनकी कुछ विशेषताएँ हैं। माना जाता है कि मिनोआई लोग हिन्द-यूरोपीय नहीं थे और न ही उनका यूनान के मुख्य भाग में रहने वाले प्राचीनवासियों से कोई सम्बन्ध था। यह अपनी अलग मिनोआई भाषा बोलते थे जो हिन्द-यूरोपीय भाषा परिवार की सदस्य नहीं थी, जबकि यूनानी भाषा इस परिवार की सदस्य है। वह जिस लिपि का प्रयोग करते थे उसे आजकल रेखीय ए (लीनियर ए) कहा जाता है और भाषावैज्ञानिक अभी तक उसे पढऩे में अक्षम रहे हैं। कांस्य युग में मिनोआई संस्कृति यूनानी सभ्यता से बहुत अधिक विकसित थी। इतिहासकारों का मानना है कि सन् 1450 ईपू के आसपास क्रीत में कोई भयंकर प्राकृतिक विपदा आई। संभव है की यह एक भूकंप था या फिर समीप के सान्तोरिनी द्वीप पर स्थित थेरा ज्वालामुखी का विस्फोट था। मिनोआई सभ्यता के बहुत से क्षेत्र इस से ध्वस्त हो गए हालांकि क्नोसोस का महल साबुत बच गया। इसके बाद लगभग सौ वर्षों तक यह सभ्यता लडख़ड़ाती हुई जारी रही लेकिन फिर इसका पतन शुरू हो गया। पूर्वी क्रीत में पहाड़ों के बीच एक कर्फ़ी (Καρφί) नामक स्थल मिला है जहाँ माना जाता है कि लौह युग तक कुछ मिनोआई लोग शरण लेकर फैलती हुई यूनानी सभ्यता से छुपे हुए थे।
(3) मिस्र की सभ्यता : यह विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है जो कि नील नदी के किनारे, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका के आसपास विकसित हुई है। इस सभ्यता की विशेषता है पिरामिडों का निर्माण। प्राचीन मिस्र का धर्म एक मूर्तिपूजक और बहुदेववादी मान्यताओं और अनुष्ठानों की एक जटिल प्रणाली थी जो प्राचीन मिस्र की संस्कृति का अभिन्न अंग थी। यह कई देवताओं के साथ मिस्रवासियों की बातचीत पर केंद्रित था, जिनके बारे में माना जाता है कि वे दुनिया में मौजूद हैं और उनके नियंत्रण में हैं। लगभग 1500 देवता ज्ञात हैं। मिस्र की मान्यता के अनुसार, इस ब्रह्मांड में तीन प्रकार के संवेदनशील प्राणी रहते थे- एक थे देवता; दूसरी मृत इंसानों की आत्माएं थीं, जो दिव्य क्षेत्र में मौजूद थीं और जिनके पास देवताओं की कई क्षमताएं थीं; जीवित मनुष्य तीसरी श्रेणी थे, और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण फिरौन था, जिसने मानवीय और दैवीय क्षेत्रों को जोड़ा। ईसाई धर्म और बाद में इस्लाम के राजधर्म बनने के बाद इसपर प्रतिबंध लगा दिया।
(4) मेसोपोटामिया की सभ्यता : आधुनिक इराक और ईरान, सीरिया, कुवैत और तुर्की के कुछ हिस्सों के अनुरूप फैला हुआ, नदियों के बीच विकसित, मेसोपोटामिया की सभ्यता 3000 से 600 ई. पू. के बीच मानी जाती है। मेसोपोटामिया के लोग शम्स (सूर्य देवता), अनु (आकाश देवता), एनलिल (वायु देवता) तथा नन्नार (चंद्र देवता) आदि अनेक देवी-देवताओं को पूजते थे। बेबीलोन के निवासी विशेष रूप से ‘माईक’ और असीरिया के लोग ‘असुर’ (अस्सुर) नामक देवता की उपासना करते थे। प्रत्येक नगर में एक प्रधान मन्दिर होता था। वहाँ का देवता नगर का संरक्षक देवता माना जाता था। नगर के संरक्षक देवता के लिए नगर के पवित्र क्षेत्र में किसी पहाड़ी पर या ईंटों के बने चबूतरे पर मंदिर का निर्माण किया जाता था, जिसे ‘जिगुरत’ या ‘जिग्गूरात’ कहते थे। लोग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भेड़-बकरी आदि पशुओं की बलि चढ़ाते थे। वे ज्योतिषियों, पुरोहितों, भविष्यवाणियों, जादू-टोनों तथा भूत-प्रेत आदि पर बहुत विश्वास रखते थे। बाढ़, अकाल तथा महामारी को वे देवता का प्रकोप मानते थे। नैतिकतापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। झूठ बोलना, घमण्ड करना तथा दूसरे को अप्रसन्न करने इत्यादि दुर्गुणों से दूर रहते थे। इस सभ्यता के लोग परलोक के स्थान पर इहलोक की चिंता अधिक करते थे। उनका विश्वास था कि परलोक अंधकार और दुर्भिक्ष (अकाल) का डेरा है, जहाँ पेट भरने के लिए केवल मिट्टी मिलती है।
(5) फारस की सभ्यता : आधुनिक इराक, अर्मेनिया, तुर्की, अजऱबैजान, अफग़ानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताज़ाकिस्तान, मध्यपूर्व, मिस्र आदि के क्षेत्रों में, फारस की सभ्यता 550 से 330 ई.पू. के बीच विकसित हुई है। फ़ारस का साम्राज्य कई बार विशाल बन गया और फिर ढह गया। एक समय इसका विस्तार मध्य यूरोप से लेकर भारत के पश्चिमी छोर तक तथा मध्य एशिया से लेकर मिस्र तक था। प्राचीन फारस (आज का ईरान) जब पूर्वी यूरोप से मध्य एशिया तक फैला एक विशाल साम्राज्य था, तब पैगंबर जरथुस्त्र ने एक ईश्वरवाद का संदेश देते हुए पारसी पंथ की नींव रखी। जरथुस्त्र व उनके अनुयायियों के बारे में विस्तृत इतिहास ज्ञात नहीं है। पहले सिकंदर की फौजों ने तथा बाद में अरब के आक्रमणकारियों ने प्राचीन फारस का लगभग सारा मज़हबी एवं सांस्कृतिक साहित्य नष्ट कर डाला था। आज हम इस इतिहास के बारे में जो कुछ भी जानते हैं, वह ईरान के पहाड़ों में उत्कीर्ण शिला लेखों तथा वाचिक परंपरा की बदौलत है। 1935 में रजाशाह पहलवी ने तत्कालीन फारस का नाम बदलकर ईरान कर दिया। इसके निवासियों के संयुक्त रूप से फारसी कहते हैं, यद्यपि इसके निवासियों में जातीय विविधता है। पारसी पंथ, जऱथुष्ट्री पंथ अथवा ज़ोरोएस्ट्रिनिज़म ज़न्द अवेस्ता नाम के ग्रन्थ पर आधारित है। जोरोएस्ट्रिनिइजम दुनिया के सबसे पुराने एकेश्वरवादी धर्मों में से एक है। प्राचीन ईरानी साम्राज्यों के यह राज्य धर्म, 633-654 के फारस की मुस्लिम विजय और पारसी लोगों के बाद के उत्पीडऩ के बाद 7वीं शताब्दी सीई से, इसमें गिरावट आई। अनुमानों में पारसी की वर्तमान संख्या लगभग 1,10,000-1,20,000 है, जिसमें से अधिकांश भारत, ईरान और उत्तरी अमेरिका में रहते हैं; माना जाता है कि उनकी संख्या निरंतर घट रही है। पारसी पंथ की शिक्षा- हुमत, हुख्त, हुश्वर्त (संस्कृत में सुमत, सूक्त, सुवर्तन) अथवा सुबुद्धि, सुभाष, सुव्यवहार है। पारसी एक ईश्वर को मानते हैं, जिसे अहुरा मज़्दा (होरमज़्द) कहते हैं। अग्नि को ईश्वरपुत्र समान और अत्यन्त पवित्र माना जाता है। उसी के माध्यम से अहुरा मज़्दा की पूजा होती है। पारसी मंदिरों को आतिश बेहराम कहा जाता है। स्पेन्ता अमेशा (संस्कृत-स्पन्द अमृत) पारसी धर्म में अमृतमयी ऊर्जा का नाम है, इसके 6 रूप हैं - 3 देवता: वोहु मनह, आशा वहिष्ट, क्षत्र वैर्य (संस्कृत में सुमन:, ऋत वसिष्ठ, क्षत्र वैर्य) और 3 देवियां सपेन्त अर्मैति, हौर्वतत, अमरतत (संस्कृत में स्पन्द अरमति, सार्वत्व, अमरत्व)। पारसी विश्वास के मुताबिक अहुरा मज़्दा का दुश्मन दुष्ट अंगिरा मैन्यु (आहरीमान) है।
लेखक
Latest News
01 Oct 2024 17:59:47
ओ३म 1. सनातन की शक्ति - वेद धर्म, ऋषिधर्म, योग धर्म या यूं कहें कि सनातन धर्म के शाश्वत, वैज्ञानिक,...



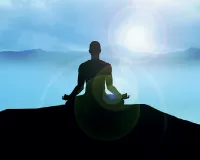


.jpg)












.jpg)
.jpg)
