आदर्श विद्यार्थी जीवन सुखमय जीवन का आधार
On

स्वामी परमार्थ देव
व्यवस्थापक-वैदिक गुरुकुलम्
संसार में सभी प्राणी सुख चाहते हैं कोई भी प्राणी दु:ख की लेशमात्र आकांक्षा नहीं करता है, चूंकि सभी प्राणियों में मनुष्य का जीवन सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए इसे सर्वोत्तम सुख की आकांक्षा स्वाभाविक रूप से बनी रहती है, परन्तु सृष्टि का अपना विधान है कि कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता। अत: यदि जीवन पर्यन्त हमको सुख की चाहना है तो उसके लिए वैसा कारण भी जुटाना पड़ेगा। आम खाना है तो आम का पौधा ही लगाना पड़ेगा, बबूल का पौधा लगाने से आम की कल्पना करना अपनी अज्ञानता का प्रदर्शनमात्र होगा। यदि हमको बहुत सुन्दर, विशाल भव्य भवन का निर्माण करना है तो उसके आधार अर्थात् उसकी नींव को बहुत ही सशक्त बनाना पड़ेगा। नींव निर्माण के बिना भवन निर्माण की कल्पना भी नहीं की जा सकती। विशाल भवन के भार को न सहने वाली नींव भवन को मिट्टी में मिला देती है, व्यक्ति का सम्पूर्ण पुरुषार्थ व्यर्थ हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से विद्यार्थी जीवन अर्थात् ब्रह्मचर्यकाल में यदि हमारा जीवन संयमित, मर्यादित, वेदानुकूल, शास्त्रनुकूल, माता-पिता, गुरु-आचार्य की आज्ञा के अनुकूल पुरुषार्थ पूर्वक विद्यार्जन नहीं होता है तथा जैसा सुना, पढ़ा जाना, अनुभव किया, वैसा आचरण नहीं करते हैं तो हमारा सम्पूर्ण जीवन सुखमय, शान्तिमय, आनन्दमय व्यतीत नहीं हो सकता। क्योंकि विद्या के बिना मनुष्य पशु के समान होता है। ‘विद्याविहीना: पशुभि: समाना:’ अत: विद्यार्थी काल में विद्या प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन, जितेन्द्रिय, अलोलुप अनासक्त, योगाभ्यास पूर्वक हर प्रकार से पुरुषार्थ करना चाहिए। विद्या प्राप्ति के विषय में कहा गया है-
आचार्योपासनाद् योगात् तपसा प्राज्ञसेवनात् ।
विगृह्य कथनात् कालात् षड्भिर्विद्या प्रपद्यते ।।
(माण्डूकीशिक्षा-179)
गुरुसेवा, योग (चित्त की एकाग्रता), तप, प्राज्ञसेवन (विद्वत्सङ्गति), विगृह्य कथन (विगृह्य सम्भाषा/शास्त्रर्थ) एवं कालक्रम (धीरे-धीरे समय बीतना, अनुभव का परिपक्व होना)- इन छ: कारणों से विद्या प्राप्त होती है। अर्थात् योग्य गुरु-आचार्य की आज्ञा का पालन व सेवा करना। अष्टाङ्गयोग का अनुष्ठान करना। विद्या अध्ययन के समय थोड़ी सर्दी-गर्मी, मान-अपमान, निन्दा-स्तुति, भूख-प्यास, सुख-दु:ख आदि सहन करना। नित्य अच्छे-सच्चे, धीर-गम्भीर विद्वानों की संगति में रहना। जो विद्या (शास्त्र) पढ़ा है उसके विषय में प्रश्नोत्तर पूर्वक परस्पर चर्चा करना तथा अध्ययन किये हुए विषय में शनै: शनै: समय बीतने पर परिपक्वता की प्राप्ति। इन छ: कारणों से विद्या की प्राप्ति होती है।
बिना शास्त्रीय ज्ञान के मनुष्य पूर्ण रूप से तनाव रहित, चिंता-मुक्त जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। वर्तमान काल में अधिकांश विद्यार्थी शास्त्रीय ज्ञान को बोझ मान बैठते हैं तथा शास्त्रीय परम्परा (गुरु-शिष्य परम्परा) को श्रद्धापूर्वक आत्मसात नहीं करते उनके लिए मंत्र, श्लोक, सूत्र स्मरण करना बहुत बड़ी चुनौती होती है। परन्तु इस सत्य तथ्य को जानकर कि विद्या जितनी बार दोहरायी जाती है उतना ही उसका विशेष लाभ होता है। स्मरण की हुई विद्या कभी निष्फल नहीं होती लोग कहावत भी कहते है ‘विद्या कण्ठ की पैसा अण्ट का’सदा मौके पर काम आता है। विद्या पारायण का फल इस जन्म में ही नहीं अगले जन्म तक भी मिलता है । यथा कहा गया है-
शतेन गुणितायाति सहस्रेण च तिष्ठति ।
शतानां च सहस्रेण प्रेत्य चेह च तिष्ठति।।
(याज्ञ- शिक्षा-0169)
एकाग्रता पूर्वक सौ बार दोहराई गई विद्या सम्यक् प्रकार से प्राप्त हो जाती है। और सहस्र (हजार) बार दोहराने से वह विद्या स्थिर (पक्की) हो जाती है तथा एक लाख बार दोहराने से तो वह इस जन्म के साथ भावी जन्म तक के लिए भी स्थिर हो जाती है। इसीलिए विद्या विलास में विद्यार्थीगण कभी भी प्रमाद न करें।
इसी रहस्य को उजागर करते हुए माण्डूकीशिक्षा में कहा गया है कि-
पदं पादं तथाद्र्धर्चं सेवितव्यं प्रयत्नत:।
अप्राज्ञ: प्राज्ञतां याति सरिद्भि: सागरो यथा।।
(माण्डूकीशिक्षा-175)
विद्यार्थी प्रतिदिन एक पद, एक पाद (चरण) अथवा भले ही आधी रचना ही याद करे, परन्तु करे अवश्य। कभी भी अभ्यास में व्यवधान न होने दे। इस प्रकार करता हुआ वह एक दिन उच्चकोटि का विद्वान् बन जाता है जैसे सब ओर से आने वाली नदियों के द्वारा सागर परिपूर्ण हो जाता है। इस संदर्भ में और भी कहा है-
ऊधर्व सहस्रादाम्नातं सततं चान्ववेक्षणम् ।
आप्तैस्तु सह सम्पाठस्त्रिविधा धारणा स्मृता।।
(माण्डूकीशिक्षा-171)
सहस्र (हजार) से भी अधिक आवृत्ति करना, निरन्तर अर्थ का अन्वेक्षण (चिन्तन) करते रहना, आप्त (पूर्ण-विद्वान्) जनों के साथ चर्चा करना- इन तीन प्रकारों से विद्या की धारणा (दृढ़ता) होती है। ऐसा आचरण करने वाला विद्यार्थी विद्वता को धारण कर जीवन में जो प्राप्त करना चाहे प्राप्त कर सकता है। क्योंकि जो विद्यार्थी अध्ययनकाल में अपनी विद्या प्राप्ति में पुरुषार्थ करते हैं तथा अनुत्पादक (निंदा, स्तुति, ईष्या-द्वेष, लड़ाई-झगड़ा, नशा करना, गप-शप, मोबाईल में अनावश्यक चैटिंग करना, कमेंट करना, मूवी देखना, गेम खेलना, इधर-उधर चक्कर काटना, शॉपिंग करना, सजना-सँवरना (मेकअप करना) आदि) कार्यों से बचते हैं, वे ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं । आदर्श विद्यार्थी का संस्कार ‘सादा जीवन उच्च विचार’होना चाहिए ।
यथा पिपीलिकाभिश्च क्रियते पांसुसञ्चय:।
न चात्र बलसामथ्र्यमुद्यमस्तत्र कारणम्।।
(याज्ञ- शिक्षा-0174)
धीरे-धीरे पिपीलिकाएं (चींटियां) भी मिट्टी का ढेर सिमचत कर लेती हैं इसमें उनका बल-सामथ्र्य कारण नहीं है, प्रत्युत निरन्तर उद्यमशीलता ही कारण है इस तथ्य को ध्यानगत रखते हुए छात्र को अध्ययन में निरन्तर उद्यमशील रहना चाहिए। इससे अल्प सामथ्र्य वाला छात्र भी विद्या में पारङ्गत हो सकता है। याज्ञवल्क्य शिक्षा में श्रेष्ठ विद्यार्थियों के लिए बहुत ही सुन्दर बात कही है-
न भोजनविलम्बी स्यान्न च नारीनिबन्धन:।
सुदूरमपि विद्यार्थी व्रजेद् गरुडहंसवत्।।
(याज्ञ- शिक्षा-0164)
छात्र को भोजनविलम्बी (भोजन के विषय में आसक्त) नहीं होना चाहिए। न ही छात्र को नारी-विषयक आसक्ति तथा छात्र को पुरुष-विषयक आसक्ति रखनी चाहिए। इस उपदेश को अपनाने वाला विद्यार्थी गरुड़ एवं हंस के समान दूर देश में जाकर भी विद्याध्ययन कर सकता है। आज के परिवेश में इस उपदेश के विपरीत आचरण करने वालों की भरमार है इसीलिए आज का विद्यार्थी किसी न किसी बीमारी से बीमार है। माता-पिता बच्चों को सुदूर सुशिक्षा हेतु विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में भेजते हैं। जो विद्यार्थी संयमित व अनुशासित नहीं होते हैं वे माता-पिता और कुलवंश की परम्परा, गौरव-गरिमा को कुचलते हैं तथा अपने झूठे अहंकार पर उछलते हैं। वे सदा उलझते ही चले जाते हैं कभी भी सुलझते नहीं। वे विद्यार्थी जीवन में भी सदैव सुख की कामना करते हैं, विलासितापूर्वक जीवन जीना चाहते हैं। परन्तु वे नहीं जानते कि निर्माण काल में यदि विलासिता या विशेष सुख की चाहना है तो जीवन अंधकारमय ही रहेगा। यदि प्रकाश चाहते हैं, जीवन का सच्चा सुख और आनन्द चाहते हैं तो विद्यार्थी काल में सुख को छोडक़र विद्या के लिए घोर तप करना चाहिए। विद्यार्थियों को यह श्लोक सदा स्मरण रखना चाहिए-
सुखार्थी चेत्त्यजेद् विद्यां विद्यार्थी चेत्त्यजेत् सुखम् ।
सुखार्थिन: कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिन: सुखम् ।।
(याज्ञ- शिक्षा-0166)
यदि कोई सुख (आरामतलबी) चाहता है, तो उसे विद्या छोड़ देनी चाहिए और यदि विद्या चाहता है तो उसे सुख छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सुखार्थी को विद्या नहीं मिलती है और विद्यार्थी को सुख नहीं मिलता है। भाव यह है कि विद्योपार्जन तपस्यासाध्य है इसलिए विद्यार्थी को बहुत सुख-सुविधाओं की कामना नहीं करनी चाहिए। तपोमय जीवन बिताते हुए ही विद्या प्राप्त करने में प्रयत्नशील रहना चाहिए।
विनयावनतस्वान्त: शुद्धाचारसमन्वित: ।
जिज्ञासु: सत्यवादी च विद्यार्थी प्रियदर्शन: ।।
विद्यार्थी को विनीत(विनम्र) मनोवृत्ति का, सदाचारसम्पन्न, ज्ञान एवं विद्या के प्रति जिज्ञासु, सत्य-मधुरभाषी तथा सुदर्शन होना चाहिए । विद्यार्थी जीवन जितना पवित्र, संयमी, सदाचारी, परोपकारी, कृतज्ञ, अनुशासित व व्यवस्थित होगा उतना ही दिव्य उसका सम्पूर्ण जीवन होगा। विद्यार्थियों का परम कर्तव्य है कि ‘सदा सर्वदा सर्वत्र’अपने से बड़ों का सम्मान करें।
अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविन:।
चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु: प्रज्ञा यशो बलम्।।
जो सदा नम्र, सुशील, विद्वान् और वृद्धों की सेवा करता है, उसकी आयु, विद्या, कीर्ति और बल ये चार सदा बढ़ते हैं और जो ऐसा नहीं करते, वे इनसे वंचित रह जाते हैं ।
आलस्यान्मूर्खसंयोगाद् भयाद्रोगनिपीडनात्।
अत्यासक्त्या च मानाच्च षड्भिर्विद्या विनश्यति।।
(माण्डूकीशिक्षा-180)
आलस्य, मूर्खसङ्गति, भय, रोगग्रस्तता, विषयों में अत्यासक्ति एवं अभिमान-इन छ: कारणों से विद्या नष्ट हो जाती है । विद्यार्थी जीवन में हम बहुत कुछ सीखते हैं, शास्त्र/विषय अध्ययन के साथ-साथ वाणी, व्यवहार का संतुलन, दिव्य स्वभाव तथा हर प्रकार की परिस्थितियों में विशेष प्रबन्धन, कला-कौशल आदि परन्तु जो विषयासक्त कमजोर, आलसी, रोगी, कुत्सित मन वाले होते हैं वे कभी भी विद्या नहीं प्राप्त कर पाते ।
पञ्च विद्यां न गृह्णन्ति चण्डा: स्तब्धाश्च ये नरा:।
अलसा रोगिणश्चैव येषां च विसृतं मन:।।
(याज्ञ- शिक्षा-0163)
पाँच प्रकार के छात्र विद्या ग्रहण नहीं कर पाते हैं-
01] चण्ड (क्रोधी) छोटी-छोटी बातों में जो उलझ जाते हैं अपने मित्रों के ऊपर तथा माता-पिता व गुरुजनों के ऊपर भी जो क्रोध करते हैं,
02] स्तब्ध (ढीठ/अकड़ू) जिसको किसी भी एक बात के लिए बार-बार बताया जाये व समझाया जाये फिर भी न माने हठ दुराग्रह करे,
03] आलसी- जो दिनचर्या करने, पढऩे तथा अन्य जीवनोपयोगी कार्यों में आलस्य करे ,
04] रोगी (किसी न किसी मानसिक, शारीरिक रोग से ग्रसित),
05] जिनका मन बिखरा रहता है या विद्या-विरोधी प्रवृत्तियों में आसक्त रहता है। जो गुमसुम रहता है, जिसके मुख-मण्डल पर कभी भी प्रसन्नता के दर्शन नहीं होते, जो तनाव में रहता है।

अध्ययन में मन न लगाकर के व्यर्थ के कार्यों (अविद्या, अज्ञानता, अधर्म, अन्याय, अविवेक पूर्ण कार्यों) में जो संलिप्त रहता है। ऐसे पाँच प्रकार के विद्यार्थियों को विद्या नहीं आ सकती और उनका जीवन भी सुखमय नहीं हो सकता।
कामं क्रोधं तथा लोभं स्वादं शृङ्गारकौतुके ।।
अतिनिद्राऽतिसेवा च विद्यार्थी ह्यष्ट वर्जयेत् ।।
01] काम अर्थात् युवकों का युवतियों के प्रति तथा युवतियों का युवकों के प्रति आसक्ति पूर्ण व्यवहार।
02] क्रोध-द्वेष
03] लोभ-द्रव्य-लालसा।
04] जिह्वा की लोलुपता।
05] स्वत: का शृंगार।
06] आमोद-प्रमोद।
07] हँसी-मजाक।
08] अधिक निद्रा तथा अध्ययन को छोडक़र अत्यधिक सेवा करना, इन आठ विद्या-प्रतिबन्धकों को विद्यार्थी सर्वथा एवं सर्वदा परिवर्जित करें ।
इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आदर्श विद्यार्थी जीवन सम्पूर्ण सुखों का आधार है, इसके अभाव में जीवन नि:सार है। प्रत्येक विद्यार्थी (छात्र व छात्रा) का परम कत्र्तव्य है कि समर्थ गुरुओं की शरणागति को प्राप्त करे तथा वेदानुकूल आचरण करता हुआ जितेन्द्रियता को प्राप्त करे। जिससे शारीरिक, मानसिक, आत्मिक व सामाजिक बल की प्राप्ति कर आत्म निर्माण से राष्ट्र निर्माण तथा विश्व-निर्माण का पवित्र कार्य कर सकें एवं सूक्ति- ‘विद्या ददाति विनयम्’को चरितार्थ कर सकें । क्योंकि कहा गया है- ‘सा विद्या या विमुक्तये।’
लेखक
Related Posts
Latest News
01 Oct 2024 17:59:47
ओ३म 1. सनातन की शक्ति - वेद धर्म, ऋषिधर्म, योग धर्म या यूं कहें कि सनातन धर्म के शाश्वत, वैज्ञानिक,...



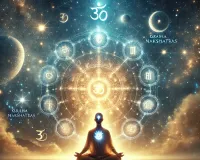




.jpg)








.jpg)
.jpg)
