मनो-शारीरिक स्वास्थ्य में आसन एवं प्राणायाम के वैज्ञानिक प्रभाव
On

डॉ. अभिषेक कुमार भारद्वाज
एसोसिएट प्रोफेसर, मनोविज्ञान विभाग, पतंजलि वि.वि. हरिद्वार
प्राण का अर्थ ऊर्जा अथवा जीवनी शक्ति है तथा आयाम का तात्पर्य ऊर्जा को नियंत्रित करना है। प्राण मन का संपोषण और संरक्षण करता है तथा विचारों को उत्पन्न करता है। अत: प्राण मन से सम्बन्धित है। महर्षि पतंजलि के अनुसार: श्वास-प्रश्वास की गति को रोकना ही प्राणायाम है।
योग एक जीवन-शैली (Way of Life) है तथा यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगी है। योग की अनेक प्रचलित पद्धतियाँ हैं जिनमें ऐसी तकनीकों का वर्णन है जो व्यक्ति के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त करती हैं। योग में शारीरिक अभ्यास, श्वसन अभ्यास, ध्यानात्मक तकनीक एवं दार्शनिक सिद्धान्त सम्मिलित हैं। योग के नियमित अभ्यास से व्यक्ति अपनी अंतर्निहित क्षमताओं तथा शक्तियों को पहचान पाने में समर्थ होता है। योग व्यक्ति में छिपी क्षमताओं को उभारता है जिससे व्यक्ति में स्वयं तथा समाज के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा होते हैं तथा नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व स्वस्थ एवं संतुलित ढंग से विकसित होता है। योग के अनेक मार्ग हैं जिनपर चलकर व्यक्तित्व की संपूर्णता को प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक मार्ग की पद्धति भिन्न है किन्तु सबका उद्देश्य एवं लक्ष्य समान है। योग अभ्यास के कुछ अंग जैसे- आसन, प्राणायाम के वैज्ञानिक प्रभाव का वर्णन अग्रांकित है -
आसन के प्रभाव (Effect of Asanas)
आसन (शारीरिक अभ्यास) का प्रभाव शारीरिक तथा मानसिक स्तर पर पड़ता है। आसन का प्रभाव शरीर के प्रत्येक अंगों, ग्रंथियों, मांसपेशियों, तंत्रिका तंत्र सहित अन्य तंत्रों पर, यहाँ तक कि कोशिकाओं पर भी पड़ता है। आसन के द्वारा शरीर के अंगों में होने वाले संकुचन तथा प्रसार से रक्त नलिकाएँ प्रभावित होती हैं और शरीर में रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है। आसन के नियमित अभ्यास से शरीर की माँसपेशियाँ चुस्त तथा लचीली (flexible) होती है। व्यक्ति के शारीरिक तथा मानसिक विकास में अंत:स्त्रावी गं्रथियों (endocrine glands) की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन ग्रंथियों से निकलने वाले हॉर्मोन का प्रभाव शारीरिक एवं मानसिक विकास पर पड़ता है। इन अंत:स्त्रावी ग्रंथियों (endocrine glands) के समुचित विकास के लिए कई आसनों को महत्त्वपूर्ण माना जाता है। आसन के अभ्यास का प्रभाव न्यूरोट्रान्समीटर के स्तर पर भी पड़ता है। एक अध्ययन में योगाभ्यासियों पर योगासन के एक सत्र (60 मिनट) के अभ्यास का प्रभाव गाबा (गामा एमिनो ब्यूटिरिक एसिड) न्यूरोट्रान्समीटर के स्तर पर देखा गया तथा गाबा स्तर में 27 प्रतिशत की वृद्धि अंकित की गयी (Journal of Alternative and Complementary Medicine, 2007) गाबा स्तर में वृद्धि चिंता की कमी से सम्बन्धित होता है।
बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उन्हें बचपन से ही कुछ आसन जैसे- सूर्य नमस्कार इत्यादि का अभ्यास कराया जाना चाहिए। शरीर में पाए जाने वाले अंत:स्रावी ग्रंथियों से जो हॉर्मोन निकलता है वह बच्चों के शारीरिक तथा मानसिक विकास में महत्वपूर्ण होता है। प्रात:काल इनका नियमित रूप से अभ्यास करने से बच्चों की स्मरणशक्ति, मेधाशक्ति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है तथा अन्य संज्ञानात्मक क्षमताएँ (तर्क शक्ति, समस्या समाधान, अवधान आदि) भी विकसित होती हैं।
योग विज्ञानसम्मत ऐसी जीवन-शैली का नाम है जिससे व्यक्ति के सम्पूर्ण जीवन में सकारात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। इससे व्यक्ति न केवल आधि व व्याधि से मुक्त होता है बल्कि इसके निरन्तर अभ्यास से समाधि की प्राप्ति भी कर सकता है। योग के सतत् अभ्यास से जीवन में रोग, शोक, चिंता, तनाव, अवसाद, आत्महीनता, मोह आदि व्यक्ति की कमजोरियाँ (मनोरोगों के लक्षण) क्रमश: समाप्त हो जाती हैं। योग व्यक्ति की कार्य-क्षमता एवं कार्य-दक्षता को बढ़ाने में भी सहायक होता है।
सूर्य नमस्कार के लाभ
-
यह एक पूर्ण व्यायाम है जिससे शरीर के प्रत्येक अंग-अवयव निरोगी होते हैं।
-
यह मेरुदण्ड एवं कमर को लचीला बनाकर सम्बन्धित विकृतियों को दूर करता है।
-
इसके अभ्यास से संपूर्ण शरीर में रक्त परिसंचरण ठीक प्रकार होता है।
-
नियमित अभ्यास से आमाशय, छोटी तथा बड़ी आँतें, यकृत (Liver), गुर्दा (Kidney), फेफड़े आदि स्वस्थ होते हैं।
-
यह अन्त:स्रावी ग्रंथियों पर क्रमश: अच्छा प्रभाव डालता है।
-
इसके नियमित अभ्यास से सजगता में वृद्धि होती है तथा अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है।
आसनों के लाभ
आसन के अभ्यास से शरीर और मन में स्थिरता आती है, रोग से मुक्ति मिलती है और अंग-प्रत्यंगों में हल्कापन आता है (हठयोग प्रदीपिका, 1/17)।
कुछ मुख्य आसनों के लाभ का संक्षिप्त वर्णन निम्न है -
-
पद्मासन: शरीर को लम्बे समय तक स्थिर रखने के लिए यह एक उत्तम अभ्यास है। शरीर के स्थिर होते ही मन शांत हो जाता है जिससे ध्यान की अनुभूति में तीव्रता आती है।
-
वीरासन: यह आसन मन को संतुलित बनाता है, एकाग्रता में वृद्धि करता है तथा मनो-शारीरिक स्तर पर विश्रान्ति प्रदान करता है।
-
शशांकासन: यह अभ्यास एड्रीनल ग्रंथि के कार्यों को नियमित करता है। शशकासन का अभ्यास मानसिक तनाव, क्रोध, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आदि को दूर करके मानसिक शान्ति प्रदान करता है।
-
मण्डूकासन: इसका नियमित अभ्यास मोटापा एवं उदर सम्बन्धी विकृतियों जैसे- कब्ज, ऐसिडिटी (अम्लपित्त) आदि में लाभदायक है। इसका अभ्यास अग्नाशय (पैन्क्रियाज) को सक्रिय कर इन्सुलिन की मात्रा को संतुलित करते हुए मधुमेह को दूर करने में सहायक है।
-
सिंहासन: इसका अभ्यास गले से सम्बन्धित समस्त रोगों जैसे- हकलाना, टॉन्सिल, आहार नली में कफ का जमना आदि में विशेष रूप से लाभकारी है।
-
कुक्कुटासन: यह अभ्यास भुजाओं एवं कंधों की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के साथ ही संतुलन एवं स्थिरता की भावना का विकास करता है।
-
भुजंगासन: इसके अभ्यास से मेरुदण्ड लचीला एवं स्वस्थ बनता है जिससे तंत्रिकाएँ सबल होती हैं और मस्तिष्क तथा शरीर के बीच संचार व्यवस्था सुगम होती है। भुजंगासन कमर दर्द एवं मोटापे से ग्रसित व्यक्तियों के लिए रामबाण अभ्यास है।
-
मकरासन: यह स्लिप-डिस्क, सर्वाइकल स्पॉण्डिलाइटिस एवं सियाटिका के लिए लाभकारी अभ्यास है।
-
मर्कटासन: इस आसन का अभ्यास कमर दर्द, स्लिप-डिस्क, सर्वाइकल स्पॉण्डिलाइटिस एवं सियाटिका दर्द में विशेष रूप से लाभदायक है।
-
शलभासन: सम्पूर्ण स्वचालित तंत्रिका तंत्र को खासकर परानुकंपी तंत्र को उद्दीप्त करने में यह अभ्यास सहायक है। शलभासन कमर दर्द एवं सियाटिका दर्द में विशेष रूप से लाभकारी है। यह मेरुदण्ड के निचले हिस्से में होने वाले सभी रोगों को दूर करता है।
-
गोमुखासन: शिथिलीकरण की प्राप्ति के लिए यह एक अच्छा अभ्यास है। इससे थकान, तनाव एवं चिंता क्रमश: कम होने लगती है।
-
सर्वांगासन: इस आसन के अभ्यास से मस्तिष्क को उचित मात्रा में रक्त पहुँचता है। यह मन को शांत करता है, भावनात्मक एवं मानसिक तनाव, भय आदि को दूर करने में सहायक है। इसके अभ्यास से थाइमस ग्रंथि भी उद्दीप्त होती है जिसके फलस्वरूप प्रतिरक्षा प्रणाली की क्षमता में वृद्धि होती है (आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बन्ध; स्वामी सत्यानन्द सरस्वती)।
-
हलासन: हलासन के अभ्यास से अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के कार्यों में सुधार आता है तथा सम्पूर्ण शरीर में रक्त संचार बढ़ता है। अर्धहलासन हमारी आँतों को सबल एवं निरोगी बनाता है तथा कब्ज, मोटापा आदि को दूर कर जठराग्नि को प्रदीप्त करता है।
-
शीर्षासन: इस अभ्यास से मस्तिष्क में रक्त-प्रवाह बढ़ता है जिससे सम्पूर्ण शरीर एवं मन को नव-जीवन प्राप्त होता है। यह अभ्यास चिंता तथा अन्य मनोवैज्ञानिक परेशानियों को भी दूर करने में सहायक है।
-
पवनमुक्तासन: यह अम्लपित्त, गठिया एवं उदरगत वायु विकार के लिए बहुत ही उत्तम अभ्यास है।
-
मयूरासन: यह अन्त:स्रावी ग्रंथियों में सामंजस्य लाता है, मनो-शारीरिक संतुलन विकसित करता है तथा पेशीय नियंत्रण को बढ़ाता है। इस अभ्यास के परिणामस्वरूप त्रिदोषों के बीच संतुलन होता है।
इस प्रकार उपरोक्त आसनों के अभ्यास से अभ्यासी को अनेक मनो-शारीरिक लाभ प्राप्त होते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य ही मानसिक स्वास्थ्य का आधार है यानि मानसिक आरोग्यता के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना आवश्यक है।
प्राणायाम का प्रभाव (Effect of Pranayama)
प्राणायाम के द्वारा व्यक्ति शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ एवं सबल होता है। प्राणायाम के द्वारा नाडिय़ों का अवरोध दूर होता है तथा यह प्राणिक शरीर को शक्तिशाली एवं मजबूत बनाता है। इससे व्यक्ति में एकाग्रता की क्षमता विकसित होती है अत: विद्यार्थियों के लिए श्वसन अभ्यास खासकर भ्रामरी प्राणायाम को अत्यधिक लाभकारी माना गया है।
मानसिक स्वास्थ्य एवं प्राणायाम: अनुसंधान आधारित साक्ष्य
प्राण का अर्थ ऊर्जा अथवा जीवनी शक्ति है तथा आयाम का तात्पर्य ऊर्जा को नियंत्रित करना है। प्राण मन का संपोषण और संरक्षण करता है तथा विचारों को उत्पन्न करता है। अत: प्राण मन से सम्बन्धित है। महर्षि पतंजलि के अनुसार: श्वास-प्रश्वास की गति को रोकना ही प्राणायाम है।
तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेद: प्राणायाम:
।।2/49, योग दर्शन।।
प्राण वायु का शरीर में प्रविष्ट होना श्वास है और बाहर निकलना प्रश्वास है। इन दोनों की गति का रुक जाना अर्थात् प्राणवायु की गमनागमन रूप क्रिया का बंद हो जाना ही प्राणायाम का सामान्य लक्षण है। यहाँ आसन की सिद्धि के बाद प्राणायाम का सम्पन्न होना बताया गया है। प्राणायाम का अभ्यास करते समय आसन की स्थिरता परम आवश्यक है। प्राणायाम के अभ्यास का न्यूरोट्रांसमीटर पर विधेयात्मक प्रभाव पड़ता है। प्राणायाम की प्रक्रिया हाइपोथैलेमस को सक्रिय कर देती है। प्राणायाम के अभ्यास के दौरान नॉरएपिनेफ्रीन की मात्रा घट जाती है तथा रक्त में डोपामाइन की मात्रा बढ़ जाती है। डोपामाइन मस्तिष्क से स्रावित होने वाला न्यूरोट्रांसमीटर है जो प्रसन्नता एवं खुशी के लिए उत्तरदायी है।
इसी तरह विभिन्न प्रकार के श्वसन अभ्यास का शरीर की अन्य महत्त्वपूर्ण क्रियाओं पर भी प्रभाव पड़ता है जैसे- हृदय की धडक़न, फेफड़े का संचालन, पाचन अंगों में रसों का स्राव। ये क्रियाएँ हमारे ऐच्छिक नियंत्रण में नहीं होती हैं। स्वायत्त तंत्रिका-तंत्र को दो भागों में विभाजित किया गया है- अनुकंपी तंत्रिका-तन्त्र (Sympathetic nervous system) तथा परानुकंपी तंत्रिका-तंत्र (Parasympathetic nervous system) । ये तंत्र एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं तथा एक दूसरे के पूरक भी हैं। शरीर को क्रियाशील बनाने का कार्य अनुकम्पी तंत्रिका-तंत्र करता है। जिस समय किसी विषम परिस्थिति का सामना करने के लिये सामान्य क्रियाओं को स्थगित करके शरीर को शक्ति की आवश्यकता होती है उस समय इसी तंत्र द्वारा वह शक्ति प्राप्त करता है। इसके विपरीत शरीर के विभिन्न भागों की सक्रियता को कम करके शारीरिक शक्ति की बचत परानुकंपी तंत्र करता है।
यद्यपि दोनों तंत्र एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं लेकिन एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। साधारणतया इनका संतुलन बना रहता है परन्तु परिस्थितियों के बदलने से असंतुलन उत्पन्न होने पर उसी के अनुसार व्यक्ति के व्यवहार में भी परिवर्तन होते हैं। जिस समय अनुकम्पी तंत्र विशेष सक्रिय हो जाता है उस समय श्वसन गति, नाड़ी गति, रक्तचाप, हृदयगति आदि बढ़ जाते हैं तथा इसके विपरीत परानुकंपी तंत्र की उत्तेजना से व्यक्ति के व्यवहार में शिथिलता आ जाती है।
मन पर नियंत्रण करने का कार्य प्राणायाम द्वारा ही सम्भव है। मन सांसारिक वस्तुओं की ओर आवृत्त होता है जब उसमें आकर्षण देखता है। लेकिन प्राणायाम से आत्म तत्व एवं आत्म विश्लेषण की क्षमता विकसित हो जाती है तो मन उस ओर आवृत्त नहीं होता है।
महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम के लाभ को इन सूत्रों के माध्यम से बताया है-
तत: क्षीयते प्रकाशावरणम् ।।2/52, योग दर्शन।।
अर्थात् प्राणायाम के अभ्यास से प्रकाश (ज्ञान) का आवरण क्षीण हो जाता है।
धारणासु च योग्यता मनस: ।।2/53, योग दर्शन।।
अर्थात् प्राणायाम के अभ्यास से मन में धारणा की योग्यता भी आती है।
प्राणिक ऊर्जा ही हमारी जीवनी शक्ति तथा रोग प्रतिरोधक शक्ति का आधार है। प्राण तथा मन में घनिष्ठ संबंध है। श्वास के नियंत्रण के साथ-ही मन पर भी नियंत्रण होता है। योग के ग्रन्थों में कहा गया है कि प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से मन की तरंगें शांत हो जाती हैं। मन की गति रुक जाती है। नाड़ी शोधन प्राणायाम से नाडिय़ों की सफाई होती है जिससे मानसिक क्रियाएँ सुचारु रूप से संभव हो सके। यह मन को शांत करता है तथा व्यवहार में सौम्यता लाता है। प्राणायाम से विचार के अनियमित प्रवाह को दिशा मिलती है। श्वास जब गहरी होती है तो मन भी शांत होता है।
प्राणायाम के लाभ
प्राण से तात्पर्य शरीर में संचार होने वाली वायु (जीवनी शक्ति) से है तथा आयाम का अर्थ नियमन (नियंत्रण) से है। इसका नियमित अभ्यास समग्र स्वास्थ्य प्रदान करता है।
-
नाड़ी-शोधन प्राणायाम: इस श्वसन अभ्यास से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध होने के कारण सम्पूर्ण शरीर का पोषण होता है। मस्तिष्क के सम्बन्धित केन्द्र उत्तेजित होकर अपनी अधिकतम क्षमता से कार्य करने लग जाते हैं। इससे मानसिक शांति, एकाग्रता एवं विचारों में स्पष्टता की प्राप्ति होती है। यह अभ्यास प्राणों में सामंजस्य लाकर प्राण शक्ति को बढ़ा कर तनाव एवं चिंता में कमी लाता है (आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बन्ध; स्वामी सत्यानन्द सरस्वती)।
-
अनुलोम-विलोम प्राणायाम: इससे शरीर में स्थित संपूर्ण नाडिय़ाँ परिशुद्ध हो जाती हैं। इसके दस दिन तक लगातार अभ्यास से स्थानिक स्मृति (रास्ते, आकृति आदि की पहचान कर पाने की क्षमता) अंक में 86 प्रतिशत की वृद्धि अंकित की गयी (Psychological Reports, 1997) । एक अध्ययन में इसके 20 मिनट के अभ्यास से चयनात्मक एकाग्रता में वृद्धि देखी गयी (Perceptual and Motor Skills, 2007) । यह अभ्यास ए.डी.एच.डी. (अवधान न्यूनता अतिसक्रियता विकार) का प्रबंधन कर एकाग्रता तथा स्मृति क्षमता को बढ़ाने में कारगर है।
-
शीतली प्राणायाम: यह अभ्यास शरीर एवं मस्तिष्क को शीतलता प्रदान करता है। कामेच्छा और तापमान नियमन से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण मस्तिष्कीय केन्द्रों को प्रभावित करता है। यह मानसिक एवं भावनात्मक उत्तेजनाओं को भी शांत करने में सहायक है (आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बन्ध; स्वामी सत्यानन्द सरस्वती)।
-
भ्रामरी प्राणायाम: इसका नियमित अभ्यास क्रोध, अनिद्रा एवं अन्य मानसिक परेशानियों को दूर करने में सहायक है। भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास से चिंता विकृति तथा घबराहट आदि का प्रबंधन संभव है। यह अभ्यास मानसिक रोगों में बहुत लाभकारी है। माइग्रेन, मानसिक उत्तेजना, मन की चंचलता को दूर कर यह स्वास्थ्य एवं शांति प्रदान करता है। ध्यान के लिए यह अत्यन्त उपयोगी अभ्यास है।
-
उज्जायी प्राणायाम: यह अभ्यास तंत्रिका तंत्र और मन को शांत करने में उपयोगी है। उज्जायी प्राणायाम थाइरॉयड, सोने के दौरान खर्राटे की आवाज, कण्ठ सम्बन्धी विकार, ज्वर आदि रोगों में कारगर अभ्यास है। यह आवाज को मधुर बनाता है। अत: इसका अभ्यास गायकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। बच्चों में हकलाने, तुतलाने की बीमारी भी इससे ठीक हो सकती है।
-
भस्त्रिका प्राणायाम: यह तंत्रिका तंत्र को संतुलित एवं मजबूत बनाता है जिससे ध्यान की तैयारी के लिए मानसिक शांति एवं एकाग्रता की प्राप्ति होती है। भस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यास से प्रतिक्रिया समय में क्रमश: कमी आती है (Indian Journal of Physiology and Pharmacology, 2003)
-
सूर्यभेद प्राणायाम: यह अभ्यास बहिर्मुखता तथा गतिशीलता में वृद्धि कर शारीरिक गतिविधियों के सम्पादन में दक्षता लाता है और अवसाद को दूर करता है। मंद बुद्धि के लोगों को या जो बाह्य वातावरण के साथ व्यवहार में या सामंजस्य बनाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, उन्हें यह अभ्यास करने का परामर्श दिया जाता है (आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बन्ध; स्वामी सत्यानन्द सरस्वती)।
उपरोक्त योगाभ्यास सावधानीपूर्वक, अपनी क्षमतानुसार तथा कुशल योग-प्रशिक्षक के निर्देशन में करना लाभकारी होता है। अभ्यासी को संबंधित आसन, प्राणायाम या अन्य अभ्यासों की सही क्रिया-विधि (जैसा कि योग ग्रंथों में वर्णित है या योगगुरु द्वारा निर्दिष्ट है), उसके वैज्ञानिक लाभ आदि का ज्ञान भी आवश्यक है। संबंधित अभ्यास किन परिस्थितियों में निषेध है या किसी असामान्य मनो-शारीरिक दशा में किस अभ्यास को नहीं करना चाहिए, इन सभी बातों की जानकारी एक योग-अभ्यासी को रखनी चाहिए।
लेखक
Related Posts
Latest News
01 Sep 2024 17:59:05
जीवन का सत्य 1. पराविद्या- मनुष्य जब ईश्वरीय सामथ्र्य अर्थात् प्रकृति या परमेश्वर प्रदत्त शक्तियों का पूरा उपयोग कर लेता...



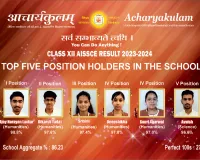
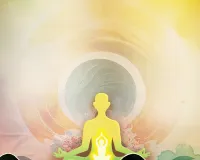
.jpg)







.jpg)
.jpg)





