पंचकर्म द्वारा कुष्ठ रोग की चिकित्सा
On

वैद्य केतन महाजन
विभागाध्यक्ष-पंचकर्म विभाग, पतंजलि आयुर्वेद हॉस्पिटल
कुष्ठ एक बहुदोष व्याधि है, जिसमें दोष अत्यधिक मात्रा में कुपित होते हैं। इसे रक्त प्रदोषज विकार तथा अष्टमहागद के अन्तर्गत लिया गया है। त्वचा में स्पर्श इन्द्रिय होने के कारण स्पर्श की अनुभूति होती है। |
त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। त्वचा को देखकर शरीर की प्राकृत तथा विकृत अवस्था का पता लगाया जा सकता है। कुष्ठ शब्द को आमतौर पर त्वचा के विभिन्न रोगों केलिए इस्तेमाल किया जाता है।
त्वच: कुर्वन्ति वैवण्र्यं दुष्टा: कुष्ठमुशन्ति तत्।। अ.हृ.नि. १४/३
जो रोग त्वचा पर तेजी से फैलने वाला तथा त्वचा के प्राकृतिक वर्ण को विकृत करने वाला होता है, उसे कुष्ठ कहते हैं।
कुष्ठ एक बहुदोष व्याधि है, जिसमें दोष अत्यधिक मात्रा में कुपित होते हैं। इसे रक्त प्रदोषज विकार तथा अष्टमहागद के अन्तर्गत लिया गया है। त्वचा में स्पर्श इन्द्रिय होने के कारण स्पर्श की अनुभूति होती है। स्पर्श इन्द्रिय पर किसी भी प्रकार का प्रभाव मन को भी प्रभावित करता है। इसलिए कुष्ठ में शारीरिक तथा मानसिक दोनों ही दोष कारण बताए गए हैं। यह मनोदैहिक रोग (Pshychosomatic Disorder) की श्रेणी में आता है।

पंचकर्म में दोषों को स्नेहन व स्वेदन द्वारा उत्क्लिष्ट करवा कर शरीर के निकटतम मार्ग (मुख, नासिका, गुदा) से बाहर निकाला जाता है। पंचकर्म के अन्तर्गत वमन, विरेचन, बस्ति (अनुवासन, निरूह), नस्य की प्रक्रियाएँ आती हैं। पंचकर्म की प्रक्रियाओं को केवल शोधन के लिए नहीं, अपितु लंघन, बृंहण, लेखन तथा शमन के लिए भी उपयोग में लाया जा सकता है।
कुष्ठ की संप्राप्ति
कुष्ठ के बताए गए निदान का अधिक मात्रा में सेवन करने से अग्रि तथा वात, पित्त, कफ- ये तीनों दोष प्रभावित होते हैं। अग्रि और त्रिदोष प्रकुपित होकर पूरे शरीर में फैलकर त्वचा, रक्त, माँस और लसिका को प्रकुपित करते हैं, जिससे क्लेद उत्पत्ति होती है। इससे त्वचा के रंग का बदलना, खुजली, दाह, राग इत्यादि लक्षण उत्पन्न होते हैं, जो शरीर के विभिन्न अंगों में कुष्ठ उत्पन्न करता है।
कुष्ठ चिकित्सा
कुष्ठ रोग की चिकित्सा उसमें पाए जाने वाले सबसे अधिक कुपित दोष के अनुसार की जाती है। कुष्ठ की चिकित्सा शुरू करने से पूर्व उसकी साध्यता या असाध्यता का भली-भाँति ज्ञान करना चाहिए।
एकदोषज, कफवातज, रसगत- सुख साध्य, वातपित्त, कफपित्त, रक्तमांसगत- कठिनता से साध्य, मेदोगत- याप्य और त्रिदोषज, अस्थि, मज्जा, शुक्रगत- असाध्य माने जाते हैं। (च.चि. ७/३८)
वातोत्तरेषु सर्पिवमनं श्लेष्मोत्तरेषु कुष्ठेषु।
पित्तोत्तरेषु मोक्षो रक्तस्य विरेचनं चाग्रे।। च.चि. ७/३९
वातप्रधान कुष्ठ में- घृतपान का सेवन, पित्तप्रधान कुष्ठ में- विरेचन तथा कफप्रधान कुष्ठ में- वमन कराया जाता है।
कुष्ठ में स्नेहपान
शोधनाङ्ग स्नेहपान- वमन, विरेचन आदि क्रियाओं से पहले शरीर में दोषों को उत्क्लिष्ट करवाने केलिए किया जाता है। कुष्ठ के स्निग्ध तथा रूक्ष दो प्रकार बताए गए हैं। रूक्ष कुष्ठ में स्नेहपान सम्यक् स्निग्ध लक्षण तक कराया जाता है, जबकि स्निग्ध कुष्ठ में स्नेहपान कोष्ठस्निग्ध लक्षण तक कराया जाता है।
कुष्ठ में स्वेदन
कुष्ठ में तीक्ष्ण स्वेदन का निषेध बताया गया है, परन्तु मन्द स्वेदन जैसे- नाड़ी स्वेदन और प्रस्तर स्वेद कुष्ठ में उसकी अवस्था और लक्षण के अनुसार प्रयोग किए जा सकते हैं। द्रव स्वेद का उपयोग भी किया जा सकता है।
कुष्ठ में शोधन
आचार्यों ने कुष्ठ में शोधन का वर्णन (अ.हृ. १९/९६) करते हुए कहा है कि १५-१५ दिन में वमन, महीने में एक बार स्रंसन, ६ महीने में रक्तमोक्षण तथा ३ दिन में नस्य करवाना चाहिये।
कुष्ठ में वमन
प्रकुपित दोषों को मुख मार्ग से बाहर निकालना वमन कहलाता है। कफप्रधान कुष्ठ, आमाशय स्थित दोष, शरीर के ऊध्र्व भाग में घाव आदि दोष तथा वसंत ऋतु में वमन कराया जाता है। वमन के लिए मदनफल, पटोल, निम्ब, कुटज आदि औषधियों का प्रयोग किया जाता है।
कुष्ठ में विरेचन
प्रकुपित दोषों को गुदा मार्ग से बाहर निकालना विरेचन कहलाता है। पित्तप्रधान कुष्ठ, अधोआमाशय स्थित दोष, पक्वाशय स्थित दोष तथा अधोदेह व्यक्त कुष्ठ में विरेचन कराया जाता है। विरेचन के लिए शरद ऋतु उत्तम मानी गई है। त्रिवृत्त, आरग्वध, दन्ति, त्रिफला आदि द्रव्यों का प्रयोग विरेचन के लिए किया जाता है। कुष्ठ में नित्य विरेचन का उल्लेख सुश्रुत संहिता में मिलता है, जहाँ अल्प बल वाले रोगी को ५, ६, ७ तथा ८ दिन तक विरेचन औषधि का प्रात:काल सेवन कराया जाता है।
कुष्ठ में बस्ति
कुष्ठ में बस्ति का निषेध बताया गया है, परन्तु जिस कुष्ठ में वात दोष प्रबल हो, बाल तथा वृद्ध में बस्ति का प्रयोग किया जा सकता है। तिक्त द्रव्यों से साधित निरुह बस्ति तथा मरिच्यादि, गुड़ुच्यादि और कायाकल्प तेल की अनुवासन बस्ति का प्रयोग किया जा सकता है।
कुष्ठ में नस्य
नासिका में औषधि को डालकर ऊध्र्व जत्रु स्थित प्रकुपित दोषों को बाहर निकालना नस्य कहलाता है। कफप्रधान, कृमिज तथा ऊध्र्व जत्रु स्थित कुष्ठ में नस्य का प्रयोग किया जाता है। सेंधा नमक, काली मिर्च, विडंग, पिप्पली आदि द्रव्यों का नस्य के लिए प्रयोग किया जाता है।
कुष्ठ में रक्तमोक्षण
दूषित रक्त को शरीर से शस्त्र तथा अशस्त्र विधियों से बाहर निकालना रक्तमोक्षण कहलाता है। पित्तप्रधान तथा रक्तप्रधान दोषों में रक्तमोक्षण किया जाता है। सिरावेध प्रच्छन्न, जलौका, शृंग, अलाबु और घटियंत्र द्वारा रक्तमोक्षण किया जाता है।
आमतौर पर कुष्ठ को दुश्चिकित्सीय कहा गया है, परन्तु शोधन के माध्यम से इस रोग के लक्षणों पर काबू पाया जा सकता है। पंचकर्म के साथ शमन औषधि, रसायन तथा पथ्य का पालन करने से कुष्ठ रोग पर नियंत्रण पाया जा सकता है।
कुष्ठ में पथ्य-अपथ्य
-
कुष्ठ रोग में घृत का सेवन, लेप, यव, गौधूम, शाली, मूँग, मसूर, शहद का सेवन लाभकारी है।
-
गन्ना, खट्टे पदार्थ, तिल, उड़द, नवीन शाली, मूली, दही, गुड़ का सेवन अहितकारी है।
-
कुष्ठ के रोगी को मैथुन, माँस तथा मद्य का सेवन त्याग देना चाहिए। पुराने चावल, मूँग, यव आदि अन्न, तिक्त रस वाला शाक हितकर होता है। (चक्रदत्त)
लेखक
Related Posts
Latest News
01 Oct 2024 17:59:47
ओ३म 1. सनातन की शक्ति - वेद धर्म, ऋषिधर्म, योग धर्म या यूं कहें कि सनातन धर्म के शाश्वत, वैज्ञानिक,...




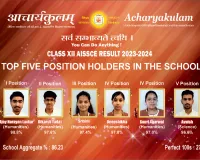

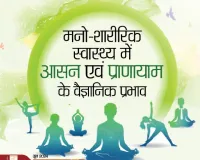













.jpg)
.jpg)
