वैदिक वाङ्मय में सामाजिक व्यवस्था
On
प्रो. महावीर जी,
प्रति-कुलपति, पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार
वैदिक साहित्य में प्रतिबिम्बित सामाजिक व्यवस्था किसी एक स्थान अथवा काल की परिधि से बंधी हुई नहीं है। वह शाश्वत् है और सार्वभौम है। युगों-युगों तक मानवमात्र का मार्गदर्शन करने की उसमें क्षमता है।
समाज शब्द सम्-उपसर्ग पूर्वक अज् (चलना) धातु से बना है। दूसरे शब्दों में मनुष्यों का एक साथ रहकर, मिलकर एक दूसरे का सहयोग करते हुए जीवन यापन करना ही समाज है। जहाँ यह सहयोग जितना अधिक होगा, सामञ्जस्य जितना सुदृढ़ होगा, उतना ही वह उन्नत समाज होगा।
वेद के अधिकांश मन्त्रों में प्रार्थना करते हुए उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया गया है। प्रसिद्ध गायत्री मन्त्र मे हम सबकी बुद्धियों को प्रेरित करने की प्रार्थना है।1 एक अन्य मन्त्र में हम सबके लिए अन्धकार से निकलकर उत्तम ज्योति सूर्य के समान ऊपर, उठने की प्रार्थना है।2 इसी प्रकार ‘हे सबका नेतृत्व करने वाले परमेश्वर (अग्ने) हम सबको उत्तम धन के लिए शोभन मार्ग से ले जाओ’।3 में सबके लिए सामूहिक प्रार्थना है, व्यष्टि के लिए नहीं है।
वैदिक ऋचाएं सब प्राणियों को अपनी आत्माओं और अपनी आत्मा को सब प्राणियों में देखने की प्रेरणा देती हैं।4 यही वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति समष्टि से एकरूप होकर घृणा से, ऊँचनीच की अलगाव की भावना से सर्वथा मुक्त हो सकता है। वेद निर्देश देता है-तुम समान मन वाले सखा होकर जागो।5
इन उत्तम भावों को प्राप्त करने की प्रथम पाठशाला है परिवार। परिवार ही वह स्थान है जहाँ मनुष्य शैशवावस्था से ही सामाजिकता को प्राप्त करता है। इसीलिए अथर्ववेद के प्रसिद्ध सौमनस्य सूक्त में माता-पिता तथा पुत्र, भाई-बहन, पति-पत्नि में पूर्ण सौमनस्य की कामना व्यत्तफ की गई है।6 वेद में ऐसे सम भाव का एवं परस्पर प्रेम का उपदेश दिया गया है जैसा गाय का अपने नवजात वत्स के प्रति होता है।7
परिवार में ग्रहण की हुई यह सौमनस्य-भावना सामाजिक जीवन में पूर्णता को प्राप्त होती है। वेद सब मनुष्यों को उसी परमपिता परमात्मा की सन्तान मानकर सब में सामाहित रहने का उपदेश देता है। ऋग्वेद में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सब मनुष्य ईश्वर के पुत्र-पुत्रियां हैं, अत: इनमें से कोई जन्म से बड़ा नहीं-और कोई छोटा नहीं, इस समानता के भाव को धारण करते हुए सब ऐश्वर्य या उन्नति के लिए मिलकर, आगे बढ़ते हैं।8
वेद के अनुसार व्यक्ति समाज का एक अंग है और इसीलिए समाज की उन्नति के लिए अपनी सम्पूर्ण शक्तियों को लगा देना सबका प्रधान धर्म है। वेद में मनुष्य के लिये ‘व्रात’शब्द का अनेक स्थानों पर प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ समुदाय अथवा संघ है। अर्थात् मानव स्वाभाविक रूप से समूह से जुड़ा हुआ है।
वैदिक समाज-व्यवस्था का दूसरा आधार है त्याग पूर्वक उपभोग।9 सामाजिक जीवन में हम एक दूसरे के लिए त्याग करने के लिए सदैव तत्पर रहें। मेरे पास जो कुछ है सब समाज ने ही दिया है। अत: आवश्यकता पडऩे पर समाज के लिए प्रिय से प्रिय वस्तु का प्रसन्नता पूर्वक त्याग करना स्वस्थ समाज की पहचान है।
वैदिक व्यवस्था में संगति का विशेष महत्त्व है किन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि इससे विविधता समाप्त हो जाये। वेद में स्वीकार किया गया है कि मनुष्य के दोनों हाथ देखने में एक समान होते हुए भी एक समान कार्य नहीं करते। सृष्टि के अस्तित्व में आने के लिए भी विषमता आवश्यक है। जब तक सत्त्व, रजस्, तमस् ये तीनों गुण साम्यावस्था में रहते हैं, तब तक सृष्टि रचना नहीं होती है। विषमावस्था के उपरान्त ही सृष्टि रचना प्रक्रिया प्रारम्भ होती है इसी प्रकार स्वभाव, संस्कार, कार्यक्षमता में भिन्नता होने पर भी एक उद्देश्य के लिए अपने-अपने स्वभाव के अनुसार मनुष्य कार्यरत रह सकता है, जिस प्रकार पृथ्वी विविध रूपों वाली होती हुई भी सब प्रकार के मनुष्यों की रक्षा करने में उसी प्रकार तत्पर रहती है जैसे एक घर के सभी सदस्य अपने घर की रक्षा करते हैं।10
इस प्रकार स्वाभाविक विषमताओं को स्वीकार करते हुए भी समान लक्ष्य का प्रतिपादन करने वाला वैदिक समाजवाद, आधुनिक ध्वंसात्मक, समाजवाद अथवा साम्यवाद से नितान्त भिन्न है, वह हृदय परिवर्तन में विश्वास करता है। यज्ञभावना, दानभावना इसका प्राण-तत्व है। वेद के अनुसार बिना बांटे अकेले भोग करने वाला व्यक्ति केवल पाप का भोग करता है।11 तैत्तिरीय उपनिषद् में भी अनेक प्रकार से दान की प्रेरणा दी गई है। मनुष्य को श्रद्धापूर्वक दान देना चाहिए, अपने सामर्थ्य के अनुसार देना चाहिए, समाज की लज्जा से देना चाहिए। भविष्य के भय से देना चाहिए, और मित्रता के लिए देना चाहिए12 वेदों में ईष्ट और आपूत्र्त का उपदेश दिया गया है। यज्ञों से वायु शुद्धि द्वारा समस्त प्राणियों का उपकार ईष्ट है और प्याऊ लगवाना, धर्मशाला बनवाना, कुएँ खुदवाना, अन्नदान, उद्यान आदि सुख, सुविधाएं प्रदान करना- ये सब पूत्र्त हैं। यह उदार-भावना उन्नत समाज का निर्माण करती है।
वेद के अनुसार, वास्तविक दाता वह है जो कृशकाय, अन्न की कामना से इधर-उधर भटकने वाले तथा दिये हुए को ग्रहण करने वाले को दान देता है।13 जो जितना अधिक दान देता है वह उतना ही अधिक यशस्वी होता है। एक चौथाई अपने पास रखकर, तीन चौथाई देने वाला उत्तम है। आधा दान देने वाला चौथाई दान देने वाले से अच्छा है और जो व्यक्ति सारा ही अपने पास रख लेता है, वह पशुतुल्य है। उसे तो आधा दान देने वाले से भी शिक्षा लेनी पड़ती है। वह बेचारा जीवन के अन्तिम क्षणों में उनके पदचिन्हों को देखता हुआ खड़ा रहता है कि कहीं कोई आकर, उसे दान का मर्म समझाये।14
दान और त्यागभावना का ही दूसरा नाम यज्ञ है। यज्ञ वैदिक सामाजिक विचारधारा का महत्त्वपूर्ण अंग है। एक मन्त्र में यह कामना व्यक्त की गई है कि मेरा प्राण, मेरा अपान, व्यान, प्रत्येक श्वास, मन, ध्यान, वाणी, निपुणता और बल सब यज्ञ भावना से युक्त हों। यह सब यज्ञ में समर्पित कर देने की उदात्त भावना है। इसकी पराकाष इस बात में है कि स्वयं याज्ञिक के यज्ञ भी यज्ञीय भावना से युक्त होने की कामना है।15 देना, सहायता करना, दु:ख दूर करना और मन से भी किसी का अशुभ न सोचना- यह यज्ञ है। उन्नत शिल्प, उन्नत उद्योग, उन्नत विज्ञान में प्रवृत्त होना भी यज्ञ है, यदि उसमें क्षुद्र स्वार्थ का त्याग किया जाये।
समस्त समाज में परस्पर मित्र-दृष्टि तथा बन्धुत्व भावना वैदिक सामाजिकता का आदर्श है। वेद में उद्घोषणा पूर्वक कहा गया है कि मैं मनुष्यों सहित सब प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखूँ। हम सब परस्पर मित्र की दृष्टि से देखें।16 अथर्ववेद में प्रार्थना की गयी है कि भगवन्! ऐसी कृपा कीजिये, जिससे मैं प्रत्यक्ष एवं परोक्ष प्राणिमात्र के प्रति सद्भावना रख सकूँ।17 हमारा आचरण इतना स्नेहपूर्ण और सहानुभूति पूर्ण हो कि कोई भी हमारे प्रति द्वेष न करे।18 हम एक दूसरे की सहायता करें। मनुष्यमात्र की सब ओर से रक्षा करें।19 इस विचार धारा में जाति, वर्ण, ऊँच, नीच, देश आदि के सब भेद समाप्त हो जाते हैं। मनुष्य की रक्षा केवल इसीलिए की जानी चाहिए क्योंकि वह मनुष्य है। यही व्यापक विश्व-परिवार की भावना है। वेद के अनुसार कर्महीन, आलसी और मानवीय गुणों से रहित व्यक्ति दस्यु है।20
वेद में विश्व-शान्ति की और सबकी स्वस्ति की स्थान-स्थान पर प्रार्थनाएं हैं।
स्वस्ति न: पथ्यासु धन्वसु स्वस्त्यप्सु वृजने स्वर्वति।
स्वस्ति न: पुत्रकृथेषु योनिषु स्वस्ति राये मरुतो दधातन।।21
शन्नो मित्र: शं वरुण: शन्नो भवत्वर्यमा।
शन्न इन्द्रो बृहस्पति: शन्नो विष्णुरुरुक्रम:।।22
वेद में समाज की कल्पना एक सुगठित शरीरधारी पुरुष के रूप में की गई है। पुरुष के विभिन्न अंगों से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चार वर्णों की उत्पत्ति बतलायी गयी है। वहाँ व्यञ्जना यही है कि जिस प्रकार शरीर के सब अंग एक दूसरे से परस्पर सम्बन्धित हैं और यदि शरीर के एक अंग में पीड़ा हो जाये तो उसका अनुभव समस्त शरीर में होता है, उसी प्रकार समाज में भी संगठन व जीवन शक्ति रहनी चाहिए।
1) धियो यो न: प्रचोदयात्।
2) उद्वयं तमसस्परि------------- सूर्यमगन्म ज्योतिरूत्तमम्।
3) अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्।
4) यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति। सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते।। वा.स. 40.4
5) उद् बुध्यध्वं समनस: सखाय: (ऋ.10.10.9)
6) अनुव्रत: पितु: पुत्रो मात्रा भवतु संमना:। जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शान्तिवाम्। मा भ्राता भ्रातरं द्विक्षन्मा स्वसारमुत स्वसा। सम्यञ्च: सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया।। (अथर्व.3.30.2.3)
7) सहृदयं सामनस्यविद्वेषं कृणोमि व:। अन्योऽन्यमभि हर्यत वत्सं जातमिवाघ्न्या।। (अथर्व.3.30.1)
8) अज्येषसो अकनिषस एते। सं भ्रातरो वावृधु: सौभगाय।। (ऋग्.5.60.5)
9) तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा:। यजु. 40.1
10) जनं बिभ्रती बहुधा विवाचसं नानाधर्मांणं पृथिवी यथौकसम्। (अथर्व. 12.1.45)
11) केवलाघो भवति केवलादी। ऋ.10.117.6
12) तै0 उ01.11
13) स इद् भोजो यो गृह्नते ददात्यन्नकामाय चरते कृशाय (ऋ.10.117.3)
14) एकपाद् भूयो द्विपदो वि चक्रमे द्विपात् त्रिपादमभ्येति पश्चात्। चतुष्पदेति द्विपदामभिश्चरे संपश्यन् पंक्तिरूपतिष्ठमान:।। ऋ.10.117.8
15) प्राणश्च मेऽपानश्च मे व्यानश्च मे--------------------वा.सं.18.29
16) मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्। मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। मित्रस्य चक्षुष समीक्षामहे। वा.सं. 36.18
17) ------ यांश्च पश्यामि यांश्च न तेषु मा सुमतिं कृधि। अथर्व.17.1.7
18) मा नो द्विक्षत कश्चन। अथर्व.12.1.24
19) पुमान् पुमांसं परिपातु विश्वत:। ऋ. 6.75.14
20) अकर्मा दस्युरभि नो अमन्तुरन्यव्रतो अमानुष:।
त्वं तस्यामित्रहन्वधर्दासस्य दम्भय।। ऋ.10.22.8
21) ऋ.10.63.15
22) ऋ.9.90.9
लेखक
Related Posts
Latest News
01 Oct 2024 17:59:47
ओ३म 1. सनातन की शक्ति - वेद धर्म, ऋषिधर्म, योग धर्म या यूं कहें कि सनातन धर्म के शाश्वत, वैज्ञानिक,...



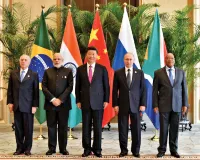


.jpg)
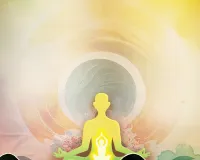










.jpg)
.jpg)
