गायत्री माता
On

महामहोपाध्याय प्रो. महावीर जी
प्रति-कुलपति, पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार
ओ३म् भूर्भुव: स्व: तत्सवितुर्वरेण्यं।
भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो न: प्रचोदयात्।।
वैदिक संस्कृति के उद्गाता ऋषियों-मुनियों और आचार्यों ने मानव जीवन में जिन-जिन की अत्यन्त गौरवपूर्ण स्थिति है, जो हम मानवों के लिये अनवरत स्नेह का झरना प्रवाहित करते हैं, जिनके बिना हमारी कोई स्थिति नहीं, उन्हें माता कहकर पुकारा है।
कृपानिधान, परमदयालु, कण-कण व्यापी, सर्वशक्तिमान्, सर्वज्ञ परमात्मा के पश्चात् संसार में जो वन्दनीय, अर्चनीय, स्नेह का सागर है, वह है माँ। माँ के आंचल में संसार का समस्त वात्सल्य कूट-कूट कर भरा हुआ हैं। ‘माता निर्माता भवति’, ‘मातृदेवो भव’ का यही अभिप्राय है। महर्षि दयानन्द सरस्वती ने अपने अमर ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश में लिखा ‘मातृमान् पितृमान् आचार्यवान् पुरूषोवेद’ पुन: ‘मातृमान्’ शब्द की व्याख्या करते हुए वे लिखते हैं-
‘प्रशस्ता धार्मिकी विदुषी माता विद्यते यस्य स: मातृमान्’ ‘जितना माता से सन्तानों को उपदेश और उपकार पहुँचता है, उतना अन्य किसी से नहीं। जैसे माता सन्तानों का हित चाहती है, उतना अन्य कोई नहीं चाहता। धन्य है वह माता कि जो गर्भाधान से लेकर जीवन भर सुशीलता का उपदेश करती रहती है।
माता के इस स्वरूप को देखकर पृथ्वी को भूमि माता, अमृत समान दुग्ध देने वाली गाय को गौ माता, ज्ञान की अजस्र धाराओं से हमारे जीवन को आह्लादित कर देने वाले वेदों को वेदमाता, देश की पवित्रतम नदी को गंगा माता, श्रीमद्भगवदगीता को गीता माता के परमपावन सम्बोधन से पुकार कर हमारा हृदय आनन्द विभोर हो जाता है, वैसे ही गायत्री मन्त्र को गायत्री माता के रूप में स्मरण करने से समस्त कल्मष प्रक्षालित होने लगते हैं। हमारी ऋषि-परम्परा ने गायत्री मन्त्र की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है। इसे नैतिकता संस्थापन में रामबाण के समान अचूक माना है। अपराधीकरण, भ्रष्टाचार और आतंकवाद के घोर अंधकार को समाप्त करने में यह मन्त्र भगवान् भास्कर की किरणों के प्रकाश पुंज के समान है। व्यष्टि, समष्टि और परमेष्टि की त्रिवेणी का यह पावन संगम है। यह ज्ञान, कर्म और भक्ति की भागीरथी है। पीडि़त, शोषित और दलित समाज के पीड़ा भंजन और उत्तरोत्तर ज्ञानवर्धन का इसमें शाश्वत् सन्देश है। सर्वतोमुखी कल्याण हेतु इसमें वर्णित अर्थ-गरिमा को जीवन में धारण करना अत्यावश्यक है। योनिश्रेष्ठ मानव जीवन की सार्थकता, शिवसंकल्पधारी मन और बुद्धि को आत्मा के अनुशासन द्वारा संयमित रखने में है।
‘गायत्री’ शब्द का अर्थ- ‘गायत्री’ एक वैदिक छन्द है। गायत्री को गुरुमन्त्र एवं महामन्त्र भी कहा जाता है। अध्ययन आरम्भ करने से पूर्व उपनयन संस्कार एवं वेदारम्भ संस्कार के समय आचार्य द्वारा ब्रह्मचारी को इस का उपदेश दिया जाता था। इस मन्त्र में विशेष रूप से बुद्धि की शुद्धता और पावनता की प्रार्थना की गई है। भविष्य के जीवन की समस्त साधना का मूलाधार यही पावनता थी। इस मन्त्र का देवता सविता है, अतएव इसको सावित्री भी कहते हैं। गायत्री में तीन अक्षर हैं। ग+य+त्र। ग- गति, य+त्र- यात्री, जिससे यात्री की गति सुगति में परिवर्तित हो जाये, वह गायत्री है।
भवसागर को पार करने के लिए गायत्री नौका का कार्य करती है। ‘गायत्री’ को प्रजापति के मुख से गीत के रूप में निकली हुई माना जाता है। जब किसी रचना में अर्थ-गरिमा रहती है, भावों की गहराई होती है, स्थायी भाव, संचारी भावों से मिलकर रसों की सृष्टि करते हैं तो गीत का जन्म होता है। कंठ से संगीत उठता है और शरीर, शरीर न रहकर गात्र हो जाता है। हृदयवीणा के तार झंकृत हो उठते हैं।
इसमें तीन महाव्याहृतियां हैं- भू:, भुव: और स्व:। व्याहृति का अर्थ है ‘वि’ विशेष रूप में ‘आ’ चारों ओर से, ‘हृ’ हरने वाली, ति- ताप।
ये तीनों महाव्याहृतियां आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक त्रिविध तापों को दूर करने वाली हैं। भू- सत् प्रकृति। भुव: चित्, आत्मा। स्व:- आनन्द, परमात्मा। ये तीनों प्रकृति, आत्मा एवं परमात्मा का बोध कराने वाली है। जब हम प्रकृति की शक्तियों को जानकर उनका विधिवत् उपयोग करना सीख लेते हैं- तो अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकम्प, अकाल आदि आधिदैविक तापों से मुक्ति मिल जाती है। आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को सम्यक् प्रकार से जाने लेने और उस आनन्दघन की उपासना में लीन रहने तथा ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने से आध्यात्मिक और आधिभौतिक दु:खों से छुटकारा मिल जाता है। रामराज्य में समस्त प्रजा इन त्रिविध दु:खों से मुक्त थी- दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। राम राज्य नहिं काहुहि व्यापा।।
महर्षि दयानन्द सरस्वती इन तीन महाव्याहृतियों का अर्थ इस प्रकार करते हैं- ‘भूरिति वै प्राण:’ ‘य: प्राणयति चराऽचरं जगत् स भू: स्वयम्भूरीश्वर:’ जो सब जगत् के जीवन का आधार, प्राण से भी प्रिय और स्वयम्भू है, उस प्राण का वाचक होके ‘भू:’ परमेश्वर का नाम है। ‘भुवरित्यपान:’ ‘य: सर्वं दु:खमपानयति सोऽपान:’ जो सब दु:खों से रहित, जिसके संग से छूट जाते हैं इसलिये उस परमेश्वर का नाम ‘भुव:’ है। ‘स्वरिति व्यान:’ ‘यो विविधं जगत् व्यानयति व्याप्नोति स: व्यान:’ जो नानाविध जगत् में व्यापक होके सबका धारण करता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम ‘स्व:’ है। ये तीनों वचन तैतिरीय आरण्यक के हैं। (सवितु:) ‘सुनोत्युत्पादयति सर्वम् जगत् स सविता तस्य’ जो सब जगत का उत्पादक और सब ऐश्वर्य का दाता है। (देवस्य) ‘यो दीव्यति-दीव्यते वा स देव:’ जो सर्व सुखों का देने वाला और जिसकी प्राप्ति की कामना सब करते हैं अतिश्रेष्ठ (भर्ग:) ‘शुद्ध स्वरूपम्’ शुद्ध स्वरूप और पवित्र करने वाला चेतन ब्रह्म स्वरूप है। (तत्) उसी परमात्मा के स्वरूप को हम लोग (धीमहि) ‘धरेमहि’ धारण करें। किस प्रयोजन के लिये कि (य:) ‘जगदीश्वर:’ जो सविता देव परमात्मा (न:) ‘अस्माकम्’ हमारी (धिय:) बुद्धियों को (प्रचोदयात्) ‘प्रेरयेत्’ प्रेरणा करे अर्थात् बुरे कामों से छुड़ाकर अच्छे कामों में प्रवृत्त करे।
हे परमेश्वर! हे सच्चिदानन्द स्वरूप! हे नित्य शुद्ध-बुद्ध मुक्त स्वभाव! हे अज निरंजन निर्विकार। हे सर्वान्तर्यामिन्! हे सर्वाधार जगत्पते! सकल जगत् उत्पादक! हे अनादे! विश्वम्भर सर्व-व्यापिन्! हे करुणामृत वारिधे! जो सब समर्थों में समर्थ सच्चिदानन्द, अनन्तस्वरूप, नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त स्वभाव वाला, कृपा सागर, ठीक-ठीक न्याय करने वाला, जन्म मरणादि क्लेश रहित, आकार रहित, सबके घट-घट का जानने वाला, सबका धत्र्ता, पिता, उत्पादक, अन्नादि से विश्व का पोषण करने वाला, सकल ऐश्वर्य युक्त जगत् का निर्माता, शुद्धस्वरूप और जो प्राप्ति की कामना करने योग्य है उस परमात्मा का जो शुद्ध चेतन स्वरूप है उसी को हम धारण करें। इस प्रयोजन के लिये कि वह परमेश्वर हमारी आत्माओं और बुद्धियों का अन्तर्यामी स्वरूप हमको दुष्टाचार अधर्मयुक्त मार्ग से हटाके श्रेष्ठाचार सत्यमार्ग में चलावे, उसको छोडक़र दूसरी किसी वस्तु का ध्यान हम लोग नहीं करें क्योंकि न कोई उसके तुल्य और न अधिक है, वही हमारा पिता न्यायाधीश और सब सुखों का देने वाला है।
भुव:
जो सब दु:खों से रहित है, जिसके संग से सब जीव सब दु:खों से छूट जाते हैं, इसलिए उस परमेश्वर का नाम ‘भुव:’ है। जो उस ‘भुव:’ का भक्त है वह पर-पीड़ा विनाश का संकल्प लेगा। मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम ने घोषणा की थी -
निसिचर हीन करउँ महि, भुज उठाइ प्रन कीन्ह,
सकल मुनिन्ह के आश्रमन्हि, जाइ-जाइ सुख दीन।’
योगेश्वर श्रीकृष्ण का उद्घोष है -
परित्रणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृताम्।
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।।
‘स्व:’
जो नानाविध जगत् में व्यापक होके सबको धारण करता है इसलिए उस परमेश्वर का नाम ‘स्व:’ है। वह सर्वव्यापक है। वह तो अन्दर ही बैठा है। उससे हम क्या छिपा सकेंगे? उसका तृतीय नेत्र सब कुछ देखता है। हम सबके अन्दर रम रहे आत्माराम के सावधान करने पर भी जब हम कुकर्मों से स्वयं को नहीं रोक पाते, तब उस कर्म का फल अवश्य प्राप्त होता है।
अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्।
यह ‘स्व:’ जीवन का मौलिक रूप है। शरीर के नाश होने पर भी उसका नाश नहीं होता। उस आत्म दर्शन से वंचित रहकर किसी का भी भला नहीं हो सकता।
तैत्तिरीय उपनिषद् के अनुसार ‘भू’ का अर्थ यह लोक अर्थात् पृथ्वी है। ‘भुव:’ का अर्थ अन्तरिक्ष लोक और ‘स्व:’ का अर्थ द्युलोक है। इन पर विचार करते हुए भक्त को यह सोचकर गौरव युक्त हो जाना चाहिए कि उसका सम्बन्ध विराट् से है।
‘सवितु:’
सब जगत् का उत्पादक और सब ऐश्वर्यों का दाता होने से परमेश्वर का नाम सविता है। वह सकल ऐश्वर्य युक्त जगत् का निर्माता है। वह अन्नादि से विश्व का भरण पोषण करने वाला है। सविता, सूर्य को भी कहते हैं। सूर्य के प्रकाश बिना मानव जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। सूर्य अपार ऊर्जा का केन्द्र है। सूर्य के उदित होते ही सम्पूर्ण सृष्टि प्रफुल्लित हो जाती है। सूर्य के अस्तोदय के माध्यम से जीवन की शिक्षा दी गई है -
उदेति सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तमेति च।
सम्पत्तौ च विपत्तौ च महतामेकरूपता।।
योगेश्वर श्रीकृष्ण गीता में अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए अर्जुन से कहते हैं -
अहं ज्योतिष्मान् अंशुमान् रवि:।
मैं ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ।
‘वरेण्यम्’
जो गुण, कर्म, स्वभाव और सत्य व्यवहारों में सबसे अधिक हो उसे श्रेष्ठ कहते हैं। उन सब श्रेष्ठों में भी जो अत्यन्त श्रेष्ठ है, उसको परमेश्वर कहते हैं, वहीं वरण करने योग्य ‘वरेण्य’ है। वही इन्द्र, विष्णु, ब्रह्मा, प्रजापति है। जब हम प्रभु को वरण कर लेते हैं, तब हम सांसारिक चिन्ताओं से मुक्त हो जाते हैं। प्रतिक्षण ऐसा अनुभव होता है, मानो वह छत्र बनकर सर्वदा रक्षा कर रहे हैं। वरण करने योग्य का वरण करने वाला उपासक वेद के शब्दों में ‘श्रिया प्रावृता: यशसा परीवृता:’ बन जाता है। सुख में, दु:ख में, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जो प्रभु हमारी रक्षा करते हैं, वे ही वरेण्य हैं।
भर्ग:
वह शुद्ध स्वरूप, पवित्र करने वाला, चेतन, ब्रह्मस्वरूप है, नित्य शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव है, निरंजन, निर्विकार है। अविद्यादि दोषों से रहित है। उस प्रकाश स्वरूप का उपासक तेजस्वी, वर्चस्वी, यशस्वी बन जाता है। वह हमारे भीतर के काम, क्रोध, लोभ आदि शत्रुओं को जलाकर भस्म करने का सामथ्र्य रखता है। भर्ग में संकल्पों का शिवत्व चाहिये। सूर्य देवता भी भर्ग स्वरूप है, सूर्योपासना इसी लिये की जाती है। सूर्य से अपार ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य राश्मियां, कीट, कीचड़, दुर्गन्ध को दूर कर देती हैं।
देवस्य धीमहि
जो सब सुखों को प्रदान करने वाला है। जिस प्रभु की प्राप्ति हेतु भक्त साधना करते हैं- ऋषिवर लिखते हैं - ‘यो मोदयति स देव:’ जो स्वयं आनन्द स्वरूप है और दूसरों को आनन्द प्रदान कराता है जिसको दु:ख का लेश भी न हो।
‘यो माद्यति स देव:’
जो सदा हर्षित, शोक रहित और दूसरों को हर्षित करने और दु:खों से पृथक् रखने वाला है, इससे उस परमेश्वर का नाम देव है। प्रतिकूलता में भी अनुकूलता की अनुभूति देवत्व है। माता, पिता, आचार्य साक्षात् देव हैं। राष्ट्र भी देव है। परहित, परोपकार में सदा रत रहने वाले मानव भी देव होते हैं। भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहूति देने वाले वीरों को हम देव मानते हैं। उस देव अर्थात् परमानन्द प्रदान करने वाले प्रभु का हम ध्यान करें, हम उसमें लीन होने का प्रयास करें। देवों की सन्निधि में रहने वाला कभी पापपंक में लीन नहीं होता, वह संसार में रहते हुए भी जनकवत् नि:स्पृह, निष्कलंक जीवन जीता है। श्रीमद्भगवद्गीता में दैवी संपद् का हृदयस्पर्शी वर्णन है -
अभयं सत्त्वसंशुद्धिज्र्ञान योग व्यवस्थिति:।
दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यास्त्तप आर्जवम्।।
अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्त्याग: शान्तिरपैशुनम्।
दया भूतेष्वलोलुपत्वं मार्दवं ह्रीरचापलम्।।
तेज: क्षमा धृति: शौचमद्रोहो नातिमानिता।
भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत।। गीता 16/1,2,3
इन गुणों से जीवन को विभूषित करना ही सबसे बड़ा ऐश्वर्य है।
धियो यो न: प्रचोदयात्
वह सविता देव परमात्मा हमारी बुद्धियों को बुरे कामों से छुड़ाकर अच्छे कामों में प्रवृत्त करे। वह सच्चिदानन्द हमें अर्थात् हमारी आत्माओं और बुद्धियों को दुष्टाचार, अधर्म युक्तमार्ग से हटाकर श्रेष्ठाचार सत्य मार्ग में चलावे। ‘बुद्धिज्र्ञानेनशुध्याति’ बुद्धि पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों के विवेक से पवित्र होती है। मानव जीवन में बुद्धि का स्थान सर्वोपरि है। ‘बुद्धिर्यस्य बलं तस्य’। बुद्धि वैभव से असंभव भी संभव हो जाता है। सात्त्विक, पवित्र, कल्याण करने वाली बुद्धि से अलंकृत मानव महर्षि दयानन्द, स्वामी विवेकानन्द, जगद्गुरू शंकराचार्य, गौतम बुद्ध, योगर्षि स्वामी रामदेव बनकर सदा-सदा के लिये अमर हो जाता है। आचार्य चाणक्य अपने बुद्धि कौशल से महानन्द को राजसिंहासन से पदच्युत कर चन्द्रगुप्त को चक्रवर्ती सम्राट् बना देते हैं।
कितना सुन्दर कहा है -
जहां सुमति तहं सम्पत्ति नाना, जहाँ कुमति तहं विपति निदाना।
प्रतिदिन इस गायत्री मन्त्र का श्रद्धा, भक्तिपूर्वक अर्थ का विचार करते हुए एकाग्र चित्त से जो ध्यान करता है, रोम-रोम से गाता है, करुणार्द्र चित्त से पुकारता है, वह अध्यात्म गंगा में स्नान करता हुआ, अपने मानव जीवन को पूर्णत: सफल बना लेता है। वेद के सन्देश- ‘मनुर्भव, जनय दैव्यं जनम्’ की पूर्णता भी गायत्रयादि की उपासना से ही संभव है।
प्रभु का ध्यान करने वाला प्रभुमय हो जाता है। विषय, भोगों का ध्यान करने वाले का जीवन ही नष्ट हो जाता है। गीता के द्वितीय अध्याय में कहा है -
ध्यायतो विषयान् पुंस: संगस्त्तेषूपजायते,
संगात्संजायते काम: कामात् क्रोधोऽभिजायते।।
क्रोधात् भवति संमोह:, संमोहात् स्मृतिविभ्रम:,
स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति।। गीता 2/62, 63
हम अपने मानव जीवन को सफल बनाने के लिये तथा सतत आनन्द सागर में डूबे रहने के लिए गायत्री माता की शरण में चलें।
लेखक
Related Posts
Latest News
01 Sep 2024 17:59:05
जीवन का सत्य 1. पराविद्या- मनुष्य जब ईश्वरीय सामथ्र्य अर्थात् प्रकृति या परमेश्वर प्रदत्त शक्तियों का पूरा उपयोग कर लेता...








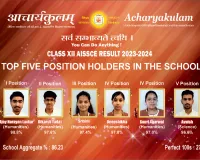





.jpg)
.jpg)





