दैनिक समग्र योगाभ्यास के लिए मुख्य 12 आसन
On

जिम तथा व्यायामशालाओं में प्रचलित शारीरिक व्यायाम से केवल मांसपेशियाँ विकसित होती हैं, जबकि आसनों के अभ्यास से शरीर के समस्त जोड़, मांसपेशियों की क्षमता, शक्ति तथा लचीलेपन में वृद्धि होती है। तरीके से श्वास-प्रश्वास को ध्यान में रखते हुए अभ्यास करने से सम्पूर्ण्ण शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता एवं रक्त-संचार में भी वृद्धि होती है। |
कमजोर शरीर, विकलाङ्ग एवं दीर्घ रोगी व्यक्ति भी समुचित मार्गदर्शन में इन आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। परम पूज्य योगर्षि स्वामी रामदेव जी महाराज द्वारा वर्षों की तपस्या तथा शोध-अनुसन्धान द्वारा प्रतिपादित अत्यन्त लाभदायी निम्रलिखित १२ आसनों का संपूर्ण पैकेज प्रस्तुत है, जिससे हर कोई लाभ उठा सकता है।
बैठकर किये जाने वाले आसन
मण्डूक आसन
विधि: वज्रासन में बैठकर दोनों हाथों की मुट्ठी बन्द करके (मुट्ठी बन्द करते समय अङ्गूठे को अङ्गुलियों से दबायें) दोनों मुट्ठीयों को नाभि के दोनों ओर लगाकर श्वास बाहर छोड़ते हुए सामने की ओर झुकते हुए दृष्टि को सामने रखकर, थोड़ी देर इसी स्थिति में रहने के बाद वापस वज्रासन में आ जायें; इस प्रकार तीन से पाँच आवृत्ति करें। यह क्रिया मण्डूकासन (प्रथम) कहलाती है।


लाभ: अग्न्याशय (पैन्क्रियाज) को सक्रिय करके इन्सुलिन की मात्रा को सन्तुलित करते हुए मधुमेह (डायबिटीज) को दूर करने में यह सहायक है। मोटापे एवं उदर से सम्बद्ध रोगों-कब्ज, एसिडिटी (अम्लपित्त) में उपयोगी है। यह हृदय के लिए भी लाभप्रद है।
मण्डूकासन-2
विधि: वज्रासन में बैठकर नाभि पर बायें हाथ की हथेली पर दायें हाथ की हथेली को रखते हुए पेट को अन्दर दबायें तथा श्वास को बाहर निकालते हुए पूर्व की भाँति (मण्डूकासन-1) धीरे-धीरे नीचे झुककर दृष्टि सामने रखना मण्डूकासन-२ कहलाता है।

लाभ: पूर्ववत्।
शशकासन
विधि: वज्रासन में बैठकर दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर उठायें, तब आगे झुकते हुए श्वास बाहर छोड़ें एवं हाथों को आगे फैलाकर हथेलियाँ नीचे की ओर रखते हुए कोहनियों तक हाथों को भूमि पर टिका दें, माथा भी भूमि पर टिका हुआ हो। कुछ समय इस स्थिति में रहकर पुन: वज्रासन में आ जायें। इस क्रियाभ्यास को 'शशकासन’ कहते हैं।

नीचे झुकते हुए यह ध्यान दें कि नितम्ब एडिय़ों से ही लगे रहें अर्थात् नितम्बों को न उठायें।
लाभ: शशकासन-आँत, यकृत्, अग्न्याशय एवं गुर्दों को ऊर्जा प्रदान करता है, स्त्रियों के गर्भाशय को पुष्ट करके उदर, कमर एवं कूल्हों की चर्बी कम करता है। मानसिक तनाव, क्रोध, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आदि को दूर करके मानसिक शान्ति प्रदान करता है। दमा व हृदय रोगियों के लिए विशेष लाभप्रद है।
वक्रासन
विधि: दण्डासन में बैठकर दायाँ और बायाँ पैर मोड़कर बायीं जङ्घा के पास घुटने से सटाकर रखें (अथवा घुटने के ऊपर से दूसरी ओर भी रख सकते हैं), बायाँ पैर सीधा रहेगा। बायें हाथ को दायें पैर एवं उदर के बीच से लाकर दायें पैर के पंजे के पास टिका दें, दायें हाथ को कमर के पीछे भूमि पर सीधा रखकर गर्दन को घुमाकर दायीं ओर कन्धे के ऊपर से मोड़कर पीछे देखें। इसी प्रकार दूसरी ओर से भी अभ्यास करना 'वक्रासन’ कहलाता है, इसे 4 से 6 बार कर सकते हैं।

लाभ: कमर व कूल्हों की चर्बी को कम करता है। मधुमेह, यकृत्, तिल्ली के लिए विशेष लाभप्रद है। कमर-दर्द के लिए उपयोगी आसन है।
गोमुखासन
विधि: दण्डासन में बैठकर बायें पैर को मोड़कर एड़ी को दायें नितम्ब के पास रखें अथवा एड़ी पर बैठ भी सकते हैं। दायें पैर को मोड़कर बायें पैर के ऊपर इस प्रकार रखें कि दोनों घुटने एक दूसरे से स्पर्श करते हुए हों। अब जो पैर ऊपर है, उसी हाथ को ऊपर से एवं नीचे वाले पैर की ओर के हाथ को पीछे कमर की ओर से ले जाकर आपस में अंगुलियाँ फँसाकर खींचें, कोहनियाँ, गर्दन व सिर सीधे रहेंगे। एक ओर से करने के बाद पुन: दूसरी ओर से भी करें। इस सम्पूर्ण क्रिया को 'गोमुखासन’ कहते हैं।
लाभ: हाइड्रोसिल (अण्डकोष वृद्धि) एवं यौन-रोगों में विशेष लाभप्रद है। स्त्री-रोगों, सन्धिवात एवं गठिया में उपयोगी है तथा लीवर, गुर्दे एवं छाती को पुष्ट करता है।
उदर के बल लेटकर किए जाने वाले आसन
मकरासन
विधि: उदर के बल लेटकर दोनों हाथों की कोहनियों को मिलाकर स्टैण्ड बनाते हुए हथेलियों को ठोड़ी के नीचे लगाकर, छाती को ऊपर उठायें। घुटनों से लेकर पंजों तक पैरों को सीधा तानकर रखें, अब श्वास भरते हुए पैरों को क्रमश: पहले एक-एक तथा बाद में दोनों पैरों को एक साथ मोड़ें, मोड़ते समय पैरों की एडिय़ाँ नितम्बों का स्पर्श करें, श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों को सीधा करना 'मकरासन’ कहलाता है।

लाभ: स्लिप डिस्क (रीढ़ की गोटियों का इधर-उधर खिसक जाना), सर्वाइकल स्पॉण्डिलाइटिस (गर्दन व उसके पीछे वाले हिस्से में दर्द का होना) एवं सियाटिका (कुल्हों का दर्द) के लिए बहुत लाभकारी अभ्यास है। अस्थमा (दमा और फेफड़े-सम्बन्धी किसी भी विकार) तथा घुटनों के दर्द के लिए विशेष कारगर है तथा यह आसन पैरों को सुडौल बनता है।
भुजङ्गासन-1
विधि: उदर के बल लेटकर हाथों की हथेलियाँ भूमि पर रखते हुए हाथों को छाती के दोनों ओर रखकर कोहनियाँ ऊपर उठी हुई तथा भुजाएँ छाती से सटी हुई होनी चाहिए। पैरों को सीधा रखकर पंजों को एक साथ मिलाकर पीछे की ओर खींचकर रखें। श्वास अन्दर भरकर छाती एवं सिर को धीरे-धीरे ऊपर उठायें। नाभि के नीचे वाला भाग भूमि पर टिका रहे, सिर व गर्दन को अधिकाधिक पीछे की ओर मोड़ें; इस स्थिति में लगभग ३० सैकेण्ड तक रुकें, तत्पश्चात् धीरे-धीरे प्रारम्भिक अवस्था में आ जायें।

भुजङ्गासन-2
विधि: उदर के बल लेटकर बायें हाथ की हथेली को छाती के नीचे रखकर उसके ऊपर दायें हाथ की हथेली रखें, माथा जमीन से लगा रहे, तब श्वास भरते हुए धीरे-धीरे सिर व छाती को ऊपर उठायें, पीछे से एड़ी-पंजे मिलाकर तानें। कोहनियों को सीधा रखते हुए हाथों को सीधा करें, इससे श्रोणि प्रदेश तक का भाग पृथ्वी से ऊपर उठ जाएगा। कुछ देर इस अवस्था में रुकें, तब धीरे-धीरे पूर्व स्थिति में आयें।

सावधानी: अत्यधिक कमर दर्द से पीडि़त व्यक्ति इस विधि को न करें। प्रारम्भ में प्रथम विधि को ही करें, धीरे-धीरे रीढ़ में लचीलापन आने पर दूसरी विधि को भी कर सकते हैं।
कमर-दर्द व मोटापे से ग्रसित व्यक्तियों के लिए यह रामबाण आसन है। मेरुदण्ड से सम्बद्ध समस्त प्रकार की विकृतियों और रोगों के लिए यह उत्तम आसन है। इससे कलाई व कन्धे सबल बनते हैं।
भुजङ्गासन-3
विधि: उदर के बल लेटकर दोनों हाथों को बगल में रखकर (भुजङ्गासन-१ की भाँति), अब आगे से सिर व छाती को ऊपर उठायें। फिर दोनों हाथों को भूमि से ऊपर उठा लें, पीछे से घुटने, एड़ी व पंजे मिले हुए तथा तने हुए रहें, इसी अवस्था में कुछ देर यथाशक्ति रुककर पुन: वापिस आएं। इस क्रिया को ३ से ५ बार दोहरायें।

शलभासन-1
विधि: उदर के बल लेटकर दोनों हाथों को जंघाओं के नीचे रखें, ठुड्डी जमीन पर लगी रहेगी। श्वास अन्दर भरकर दायें पैर को बिना घुटना मोड़े ऊपर उठाकर १० से ३० सैकेण्ड तक इस स्थिति में रहें। सामान्य स्थिति में आकर पुन: बायें पैर से अयास करें। अब दोनों पैरों को एक साथ मिलाकर बिना घुटने मोड़े हथेलियों का रुख अपनी सुविधानुसार ऊपर या नीचे की ओर रखें, (सभी अङ्गुलियाँ मिली रहेंगी) अब ऊपर की ओर उठें, इसमें नाभि से नीचे तक का भाग ऊपर उठ जाएगा। यह क्रियाभ्यास 'शलभासन-' कहलाती है।

लाभ: मेरुदण्ड के नीचे वाले भाग में होने वाले सभी रोगों को दूर करता है। कमर-दर्द एवं सियाटिका दर्द में विशेष लाभप्रद है। फेफड़े मजबूत बनते हैं, कब्ज टूटती है। यह यौन-रोगों में लाभकारी है।
शलभासन-2
विधि: उदर के बल लेटकर दायें हाथ को कान तथा सिर से स्पर्श करते हुए सीधा रखें तथा बायें हाथ को पीछे कमर के ऊपर रखकर श्वास अन्दर भरते हुए आगे से सिर एवं दायें हाथ को तथा पीछे से बायें पैर को भूमि से ऊपर उठाकर, थोड़ी देर इस अवस्था में रुककर शनै:-शनै: वापस आयें, इसी प्रकार बायीं ओर से इस आसन को करें।

शलभासन-3
विधि उदर के बल लेटकर दोनों हाथों को पीठ के पीछे ले जाकर सीधा रखते हुए, एक दूसरे हाथ की कलाइयों को पकड़ें, श्वास भरकर सिर व छाती को अधिकाधिक ऊपर उठायें (पीछे से हाथों को खींचकर रखें), दृष्टि आकाश की ओर जमी रहेगी।

लाभ: पूर्ववत्।
पीठ के बल लेटकर किये जाने वाले आसन
मर्कटासन-1
विधि: सीधे लेटकर दोनों हाथों को कन्धों के समानान्तर फैलायें, हथेलियाँ आकाश की ओर खुली रहे; फिर दोनों पैरों को घुटनों से मोड़कर नितम्ब के पास लायें। अब घुटनों को दायीं ओर झुकाते हुए दोनों घुटनों और एडिय़ों को परस्पर मिलाकर भूमि पर टिकायें, गर्दन को बायीं ओर मोड़कर रखें; इसी तरह से बायीं ओर से भी इस आसन को करें, यह 'मर्कटासन-१Ó कहलाता है।

मर्कटासन-2
विधि: पीठ के बल लेटकर दोनों पैरों को घुटनों से मोड़कर नितम्बों के पास रखें, पैरों में लगभग डेढ़ फुट का अन्तर रखें (दोनों हाथ कन्धों की सीध में फैले हुए हथेलियाँ ऊपर की ओर हों)। अब दायें घुटने को दायीं ओर झुकाकर भूमि पर टिका दें, बायें घुटने को इतना झुकायें कि वह दायें पैर के पंजे से स्पर्श करे, गर्दन को बायीं ओर अर्थात् विपरीत दिशा में मोड़कर रखें। इसी प्रकार से दूसरे पैर से भी करें।

मर्कटासन-3
विधि: सीधे लेटकर दोनों हाथों को कन्धों के समानान्तर फैलायें, हथेलियाँ आकाश की ओर खुली हों। दायें पैर को 90 डिग्री (900) उठाकर धीरे-धीरे बायें हाथ के पास ले जायें, गर्दन को दायीं ओर मोड़कर रखें, कुछ समय इसी स्थिति में रहने के बाद पैर को ९० डिग्री (९००) पर सीधे उठाकर धीरे-धीरे भूमि पर टिका दें। इसी तरह बायें पैर से इस क्रिया को करें।

अन्त में दोनों पैरों को एक साथ ९० डिग्री (९००) पर उठाकर बायीं ओर हाथ के पास रखें, गर्दन को विपरीत दिशा में मोड़ते हुए दायीं ओर देखें, कुछ समय पश्चात् पैरों को यथापूर्व सीधा करें। इसी तरह दोनों पैरों को उठाकर दायीं ओर हाथ के पास रखें। गर्दन को बायीं ओर मोड़ते हुए बायीं ओर देखें, यह एक आवृत्ति हुई।
सावधानी: जिनको कमर में अधिक दर्द हो, वे दोनों पैरों से एक साथ न करें। उनको एक-एक पैर से ही २-३ आवृत्ति करनी चाहिए।
लाभ: पेट-दर्द, दस्त, कब्ज एवं गैस को दूर करके पेट को हल्का बनाता है। नितम्ब तथा जोड़ों के दर्द में विशेष लाभदायक है।
कमर-दर्द, सर्वाइकल स्पॉण्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क एवं सियाटिका में यह विशेष लाभप्रद आसन है।
पवनमुक्तासन-1
विधि: सीधे लेटकर दायें पैर के घुटने को छाती के पास लायें, दोनों हाथों की अङ्गुलियाँ आपस में फँसाकर घुटनों पर रखें, श्वास बाहर निकालते हुए घुटने को दबाकर छाती से लगायें एवं सिर को उठाते हुए घुटने से नासिका का स्पर्श करें, कुछ देर करीब १० से ३० सैकेण्ड तक श्वास को स्वाभाविक स्थिति में रखकर अथवा बाहर रोककर, फिर पैर को सीधा कर दें। इसी प्रकार दूसरे पैर से भी इसी क्रिया को करना, 'पवनमुक्तासन-१’ कहलाता है।

पवनमुक्तासन-2
विधि: पूर्ववत् विधि को ही आगे बढ़ाते हुए अब द्वितीय स्थिति में दोनों पैरों को एक साथ परस्पर मिलाकर (पंजे तने हुए हों) समकोण अर्थात् ९० डिग्री (९००) तक उठायें; फिर घुटने मोड़कर घुटनों को छाती के पास रखें, तब दोनों हाथों से दोनों घुटनों को पकड़कर छाती को दबायें और सिर उठाकर नासिका को घुटनों से लगायें। श्वास को बाहर रोककर रखें अथवा स्वाभाविक रूप से श्वास लें। यह 'पवनमुक्तासन-२’ कहलाता है। इस क्रियाविधि को एक बार में ३ से ५ बार कर सकते हैं।

सावधानी: यदि कमर में अधिक दर्द हो तो सिर उठाकर घुटने से नासिका न लगायें, केवल पैरों को दबाकर छाती से स्पर्श करें; ऐसा करने से स्लिप डिस्क, सियाटिका एवं कमर-दर्द में पर्याप्त लाभ मिलता है।
लाभ: यह आसन उदरगत वायुविकार के लिए यह बहुत ही उत्तम है। स्त्री-रोग अल्पात्र्तव, कष्टात्र्तव एवं गर्भाशय-सम्बन्धी रोगों के लिए बहुत लाभप्रद है। अम्लपित्त, हृदयरोग, गठिया एवं कटिपीड़ा में हितकारी है, उदर की बढ़ी हुई चर्बी को कम करता है।
अद्र्धहलासन
विधि: पीठ के बल लेटकर हथेलियाँ भूमि की ओर, पैर सीधे एवं पंजे मिले हुए व तने हुए हों। अब श्वास अन्दर भरकर पैरों को ९० डिग्री (समकोण) तक धीरे-धीरे ऊपर उठाकर कुछ समय तक इसी स्थिति में स्थिर रहें, वापस आते समय धीरे-धीरे पैरों को नीचे भूमि पर टिकायें, झटके के साथ नहीं। कुछ विश्राम कर, फिर यही क्रिया करें, इसे 'अद्र्धहलासनÓ कहते हैं। इसे ३ से ६ बार करना चाहिए।

सावधानी: जिनको कमर में अधिक दर्द रहता हो, वे एक-एक पैर से क्रमश: इस आसन का अभ्यास करें, दोनों पैरों से एक साथ अभ्यास न करें।
लाभ: यह आसन आँतों को सबल एवं निरोग बनाता है, तथा कब्ज, गैस, मोटापा आदि को दूर कर जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। नाभि का डिगना, हृदयरोग, पेट दर्द एवं श्वासरोग में भी उपयोगी है। एक-एक पैर से क्रमश: रुकने पर कमरदर्द में विशेष लाभप्रद है।
पादवृत्तासन-1
विधि: सीधे लेटकर दायें पैर को उठाकर शून्याकृति बनाते हुए घड़ी की दिशा में ५ से १० आवृत्तियाँ करें। एक दिशा में घुमाने के बाद दूसरी दिशा में पैर को घड़ी की विपरीत दिशा (एण्टी क्लॉकवाइज) में वृत्ताकार घुमायें, तब दूसरे पैर से भी ठीक इसी प्रकार अयास करें। यह पूरी क्रिया 'पादवृत्तासन-१’ कहलाती है।

पादवृत्तासन-2
विधि: एक-एक पैर से करने के पश्चात् दोनों पैरों से एक साथ इस अयास को करें, पैरों को ऊपर-नीचे, दायें एवं बायें चारों ओर जितना ले जा सकते हैं, उतना ले जाते हुए घुमायें। दोनों पैरों से दोनों दिशाओं से अर्थात् वामावत्र्त (क्लॉकवाइज) तथा दक्षिणावत्र्त (एण्टी क्लॉकवाइज) घुमाने की क्रिया 'पादवृत्तासन2' कहलाती है।
जङ्घा, नितम्ब एवं कमर के बढ़े हुए मेद को निश्चित रूप से दूर करता है, तथा उदर को हल्का व सुडौल बनाता है। शरीर के सन्तुलन के लिए यह बहुत उपयोगी है।
द्वि-चक्रिकासन-1
विधि: पीठ के बल लेटकर हाथों के पंजे नितम्बों के नीचे रख श्वास रोककर एक पैर को पूरा ऊपर उठाकर घुटने से मोड़कर एड़ी नितम्ब के पास होकर गोलाकार (साइकिल चलाने की तरह) घुमाते रहें। इसी प्रकार दूसरे पैर से इस क्रिया को करें। पैरों को बिना जमीन पर टिकाये घुमाते रहें, पैरों से वृत्ताकृति बनायें, इस सम्पूर्ण क्रियाभ्यास को 'द्वि-चक्रिकासन-' कहते हैं। 10 से लेकर यथाशक्ति 25-.30 बार इसकी आवृत्ति करें। थक जाने पर शवासन में थोड़ी देर विश्राम करके इसी अभ्यास को विपरीत दिशा से दोहरायें।

द्वि-चक्रिकासन-2
विधि: इसी क्रिया के द्वितीय चरण में दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए घुटनों को छाती पर सटा दें, अब श्वास लेने तथा छोडऩे की क्रिया के साथ दोनों पैरों को (साइकिल के पैडल घुमाने की भाँति) वामावत्र्त घुमाइये, यही क्रिया दक्षिणावत्र्त में भी दोहराना द्वि-चक्रिकासन-2 कहलाता है।
कमरदर्द, हृदयरोग, उच्च रक्तचाप और हर्निया से ग्रसित व्यक्ति इस दूसरी अवस्था का अभ्यास न करें।

मोटापा घटाने के लिए यह सर्वोत्तम आसन है, नियमित रूप से 5 से 10 मिनट तक इसका अभ्यास करने से निश्चित ही अनावश्यक भार कम हो जाता है। उदर को सुडौल बनाता है, आँतों को सक्रिय करता है। कब्ज़, मन्दाग्नि, अम्लपित्त, धरन आदि की निवृत्ति करता है। यह सम्पूर्ण शरीर में रक्त-संचारण को तेज करके रक्तशुद्धि करता है।
इन निरापद आसनों को अपनी दिनचर्या में स्थान देकर हर कोई सुदृढ़ जीवन का स्वामी बन सकता है, तो आइये आज से ही इसके लिए संकल्पित हों।
लेखक
Related Posts
Latest News
01 Sep 2024 17:59:05
जीवन का सत्य 1. पराविद्या- मनुष्य जब ईश्वरीय सामथ्र्य अर्थात् प्रकृति या परमेश्वर प्रदत्त शक्तियों का पूरा उपयोग कर लेता...



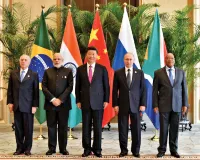
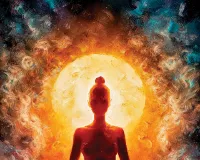
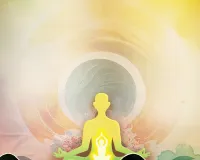




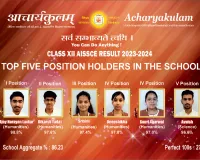



.jpg)
.jpg)





